Best Destination For CGPSC, VYAPAM
We are giving you the best approach to your success for competitive examinations like CGPSC & VYAPAM

MORE THAN 1,300 CUSTOMERS TRUST EDUMA







Affairs Current
छत्तीसगढ़ का इतिहास
March 14, 2024
No Comments
छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक युग से गुप्त काल तक प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था।छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख...
Read More »
छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश
March 14, 2024
No Comments
छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणकोशल के नाम से जाना जाता था और...
Read More »
मराठों के अधीन छत्तीसगढ़
March 14, 2024
No Comments
1742 में मराठा कमांडर भास्कर पंत ने इस क्षेत्र पर हमला किया और हैहाई राजवंश को समाप्त कर दिया। बदलती ऐतिहासिक घटनाओं में भास्कर पंत...
Read More »
छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमींदारियाँ
March 14, 2024
No Comments
छत्तीसगढ़ के पूर्व बहुमूल्य राज्य और जमींदारियाँ छत्तीसगढ़ राज्यों का विलय 15 छत्तीसगढ़ राज्य थे, उनमें से सबसे बड़ा बस्तर है जिसका क्षेत्रफल 15029 वर्ग...
Read More »
छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन
March 14, 2024
No Comments
छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन अंग्रेजों से पहले के विभिन्न शासकों का संक्षिप्त परिचय: 21वीं सदी का राज्य छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया।...
Read More »
छत्तीसगढ़ में सामंती राज्य
March 14, 2024
No Comments
छत्तीसगढ़ में सामंती राज्य:—- छत्तीसगढ़ क्षेत्र का इतिहास लगभग चौथी शताब्दी का है, जब इसे दक्षिणी (या दक्षिण) कोसल के नाम से जाना जाता था।...
Read More »
What to expect from Competition Success
Highly Experienced
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
Question, Quiz & Course
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
Dedicated Support
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur

LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you.
- Bennett Cu
/ Front-end Developer

LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you.
- Bennett Cu
/ Front-end Developer

LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you.
- Bennett Cu
/ Front-end Developer
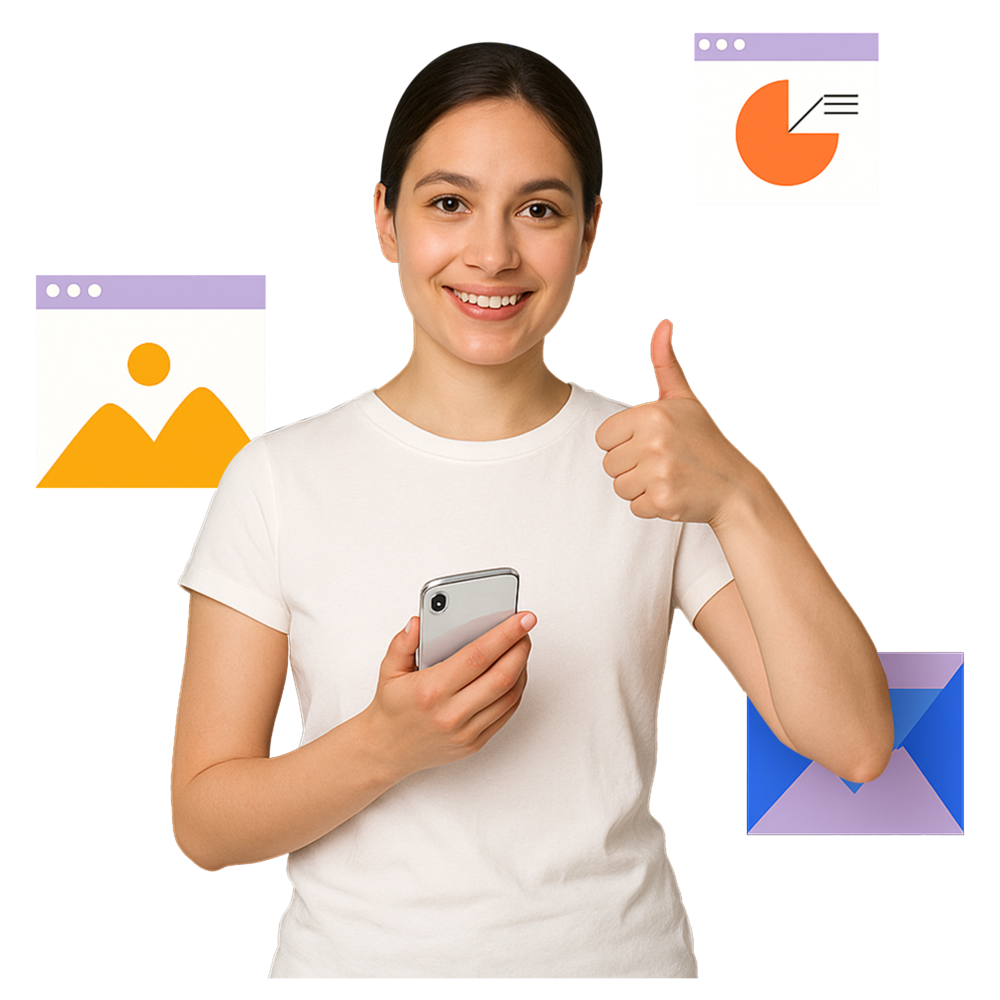
Master Every Exam Success is Just a Tap Away
No more long commutes or heavy books – study anywhere, anytime, and stay ahead with smart online learning tools.
Events Our
Upcoming Education Events to feed your brain.
11September
Vyapam Fast-Track Test Series & Strategy Meet
Lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor...
12:00 am - 12:00 am
Raipur, Chhattisgarh India
24September
Career in State Services – Free Orientation & Scholarship Test
Lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor...
12:00 am - 12:00 am
Raipur, Chhattisgarh, India
29December
CGPSC Success Bootcamp
Lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor...
12:00 am - 12:00 am
Raipur, Chhattisgarh, India
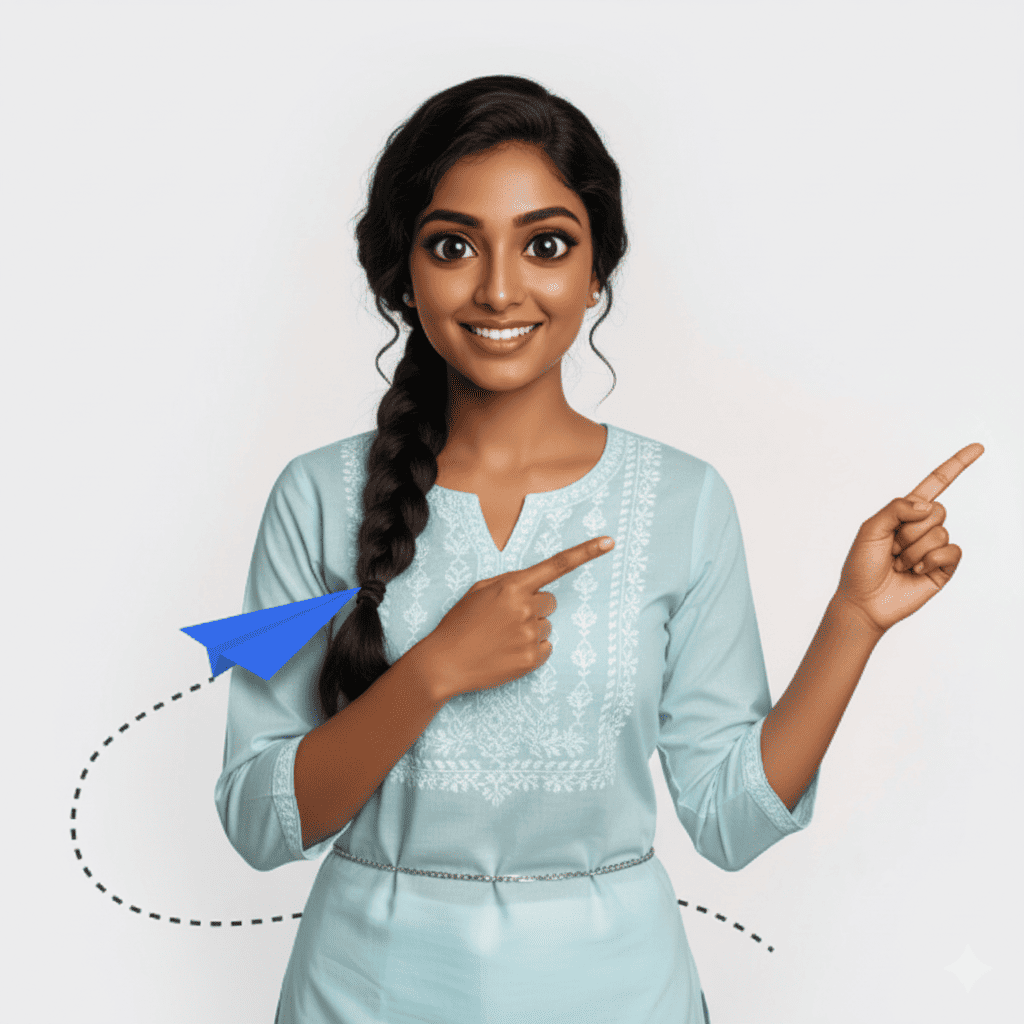
Become One Of Top Government Officer
With Us
Let's roll up our sleeves for the dream journey















