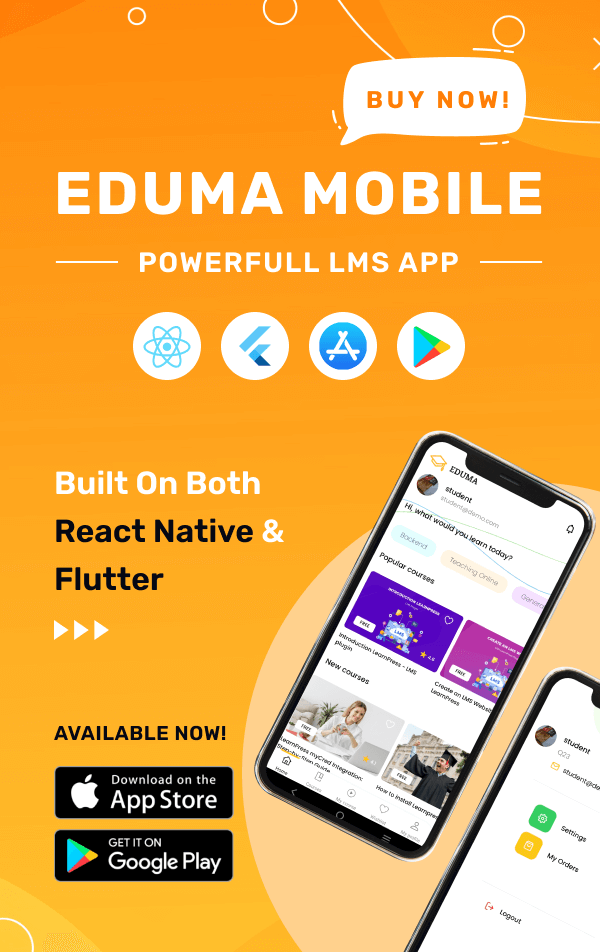संविधान में संशोधन संसद द्वारा किए जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। एक संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो बार पारित किया जाना चाहिए।
ओ-तिहाई बहुमत और मतदान। इसके अलावा, संविधान की संघीय प्रकृति से संबंधित कुछ संशोधनों को अधिकांश राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जून 2013 तक संसद में 118 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 98 पारित होकर संशोधन अधिनियम बन गए हैं।
संविधान में संशोधन
1951 जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए। एक नया संवैधानिक उपकरण, जिसे अनुसूची 9 कहा जाता है, उन कानूनों की रक्षा के लिए पेश किया गया जो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। ये कानून संपत्ति के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण करते हैं।
1953 प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार 650,000 और 850,000 मतदाताओं के बीच तय करने के लिए एक तकनीकी संशोधन।
1955 लोकसभा में 500 सदस्यों की सीमा, एक निर्वाचन क्षेत्र का एक सदस्य 500000 से 750000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
1955 संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयकों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करना।
1955 क्षेत्रीय मामलों में संशोधन और राज्य के पुन: नामकरण से संबंधित मामलों में संबंधित राज्यों के साथ परामर्श तंत्र का प्रावधान करता है।
1956 करों में वृद्धि के संबंध में संघ और राज्य सूचियों में संशोधन।
1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वर्ग ए, बी, सी, डी राज्यों का उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।
1960 निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण और अधिग्रहण की राज्य की शक्ति को स्पष्ट करें और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करें।
1960 सीमावर्ती गांवों के सीमांकन आदि द्वारा विवादों के निपटारे के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय संघ के क्षेत्र में मामूली समायोजन।
1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दादरा, नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
1961 संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।
निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को चुनौती से बचाना।
1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
1963 अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।
1962 पांडिचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण किया गया।
1963 में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई और न्यायाधीशों आदि से संबंधित नियमों की व्याख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए अन्य छोटे संशोधन किए गए।
1963 सार्वजनिक पद के इच्छुक लोगों के लिए भारतीय गणराज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेना और विभिन्न अनिवार्य प्रारूप निर्धारित करना अनिवार्य बना दिया गया।
1964 सम्पदा के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करने और भूमि अधिग्रहण कानूनों को संविधान की अनुसूची 9 में रखने के लिए
1966 में अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए तकनीकी संशोधन और इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति दी गई।
1966 चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त किया गया और नियमित उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को सक्षम बनाया गया।
1966 न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णयों, डिक्री, आदेशों और वाक्यों को क्षतिपूर्ति और मान्य करना और कुछ न्यायाधीशों को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, उनकी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति और स्थानांतरण को मान्य करना था। नियुक्तियों को अमान्य करने वाले निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ न्यायाधीशों की।
1967 सिंधी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया।
1969 असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।
1970 संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 1980 तक बढ़ाया गया।
1971 संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों को कमजोर करने में सक्षम बनाना।
1972 राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर कब्ज़ा करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवज़े को प्रतिबंधित करना।
1971 भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स की समाप्ति।
1972 मिजोरम को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया।
1972 स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त लोगों के लिए इसे एक समान बनाने के लिए सिविल सेवा नियमों को तर्कसंगत बनाया गया।
1972 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया।
1973 सिविल मुकदमों के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के आधार को मूल्य मानदंड से बदलकर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले मानदंड में बदल दिया गया।
1973 संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 सीटें। पूर्वोत्तर भारत में बने नए राज्यों में बढ़ी हुई सीटें और 1971 के परिसीमन अभ्यास के परिणामस्वरूप मामूली समायोजन।
1974 आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण।
1974 संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इस्तीफे की प्रक्रिया और सदन अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
1974 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया।
1975 सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने के लिए नियम और शर्तें।
1975 भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।
1975 अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।
1975 अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाता है
1975 का संशोधन संसद में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करने के लिए बनाया गया था। संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के पद की न्यायिक जांच पर प्रतिबंध लगा दिया।
1976 संसद को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने और खनिज संपदा को भारत संघ में निहित करने में सक्षम बनाना
भूमि सुधार और अन्य अधिनियमों तथा इन अधिनियमों में संशोधनों को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखें।
1976 संघ और राज्य लोक आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई।
1977 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान संशोधन पारित किया गया। भारत को “समाजवादी धर्मनिरपेक्ष” गणराज्य बनाकर मौलिक अधिकारों में कटौती, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और संविधान की मूल संरचना में बदलाव का प्रावधान करता है।
देश में आंतरिक आपातकाल को रद्द करने के बाद 1978 का संशोधन पारित हुआ। संशोधन विधेयक 42 के माध्यम से अधिनियमित कुछ अधिक ‘स्वतंत्रता-विरोधी’ संशोधनों को निरस्त करता है।
देश में आंतरिक आपातकाल को रद्द करने के बाद 1979 का संशोधन पारित हुआ। कार्यकारी और विधायी प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानवाधिकार सुरक्षा उपाय और तंत्र प्रदान करता है। संशोधन विधेयक 42 में अधिनियमित कुछ संशोधनों को रद्द करता है।
1980 संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 1990 तक बढ़ाया गया।
बिक्री कर पर दायरे और प्रयोज्यता पर न्यायिक घोषणाओं को नकारने के लिए 1983 में संशोधन।
1984 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया।
1985 पंजाब राज्य में दो साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
1984 त्रिपुरा को एक जनजातीय राज्य के रूप में मान्यता देना और एक त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को सक्षम बनाना।
1984 संपत्ति और संचार बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 33 में निर्धारित भाग III के अनुसार मौलिक अधिकारों में कटौती के लिए तकनीकी संशोधन।
1986 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें।
1985 दलबदल विरोधी कानून – एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दलबदल के मामले में संसद और विधानसभा से सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है।
1987 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
1986 भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना भविष्य में वृद्धि निर्धारित करने का प्रावधान।
1987 अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणामस्वरूप राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ।
1987 गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान।
1987 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया।
1987 आज की तारीख में संविधान का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान और भविष्य के संशोधनों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान।
1988 पंजाब राज्य में तीन साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया, पंजाब राज्य में या पंजाब राज्य के विशिष्ट जिलों में आपातकाल लगाने की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359ए में संशोधन किया गया।
1988 प्रोफेशन टैक्स अधिकतम रु. से बढ़ाया गया। 250/- अधिकतम रु. 2500/-.
1989 मतदान के अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गयी।
1989 संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2000 तक बढ़ाया गया।
1990 संशोधन 59 के अनुसार अनुच्छेद 359ए में दी गई पंजाब राज्य पर लागू आपातकालीन शक्तियां निरस्त कर दी गईं।
1990 पंजाब राज्य में तीन साल और छह महीने तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और इसकी वैधानिक शक्तियां संविधान में निर्दिष्ट की गईं।
1990 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया।
1990 पंजाब राज्य में चार साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
1991 पंजाब राज्य में पांच साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
1992 संघीय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करना। दिल्ली अब भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है.
1991 राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया गया।
1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया।
1992 त्रिपुरा राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें।
1993 गांवों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में पंचायत राज के लिए वैधानिक प्रावधान।
1993 कस्बों और शहरों जैसे शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान। (नगर पालिकाएँ)
1994 किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान।
1994 संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण जारी रखने को सक्षम बनाया गया।
1995 पदोन्नति में एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण की सुरक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
1995 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया।
2000 संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया गया।
2000 राज्यों और केंद्र के बीच सभी करों को एकत्रित और साझा करके कर संरचनाओं को सरल बनाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करें।
2000 रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में एससी/एसटी आरक्षण की रक्षा करें।
2000 एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में अर्हता अंक और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति।
2000 अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण से छूट।
2002 संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1991 की राष्ट्रीय जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग बढ़ाया गया।
2002 एससी/एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
2002 चौदह वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार और छह वर्ष की आयु तक बचपन की देखभाल का अधिकार प्रदान करता है।
2003 संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग बढ़ाया गया।
2004 सेवा कर लगाने और उपयोग के लिए वैधानिक कवर का विस्तार करना।
2003 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया।
2003 बोडोलैंड क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण।
2004 मंत्रिपरिषद का आकार 15% विधायी सदस्यों तक सीमित करना और दल-बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना।
2004 सेवा कर लगाने को सक्षम करें। बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करें।
2006 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण
2006 नव निर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान करना।
2010 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण साठ से बढ़ाकर सत्तर साल कर दिया गया।
2011 ने आठवीं अनुसूची में “उड़िया” को “उड़िया” में बदल दिया।
2012, 12 जनवरी यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। (19(1)सी)
सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। (43बी)
सहकारी समितियाँ. (भाग 9बी)
2013, 2 जनवरी हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना।
(संविधान में अनुच्छेद 371जे सम्मिलित करना)