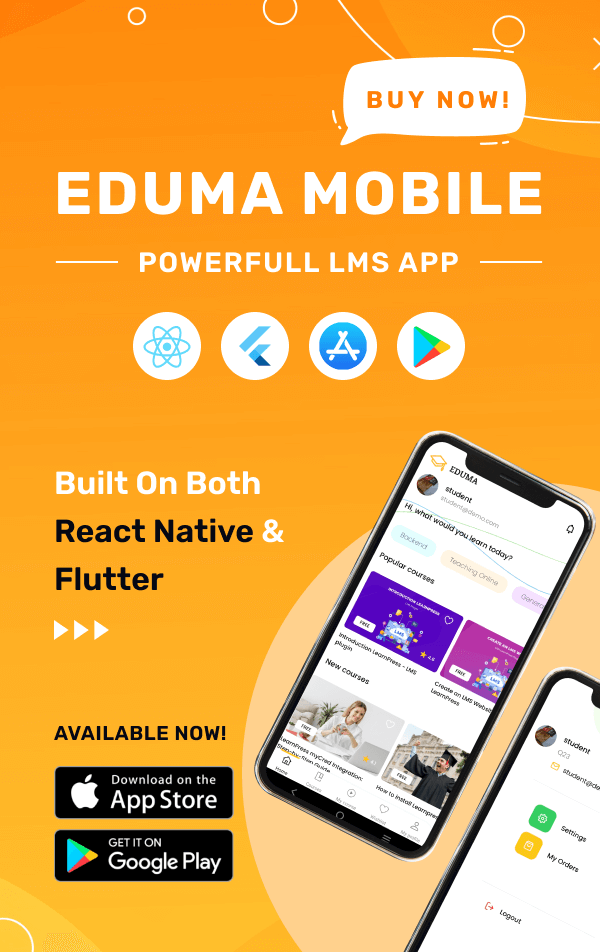बुनियादी संरचना
मूल संरचना सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है कि भारत के संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन “बुनियादी विशेषताओं” में से प्रमुख हैं संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार। इस प्रकार यह सिद्धांत संसद द्वारा अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की सीमित शक्ति का आधार बनता है जो संविधान की इस “बुनियादी संरचना” के साथ संघर्ष करते हैं या इसे बदलने की कोशिश करते हैं।
1965 में, “बुनियादी विशेषताएं” सिद्धांत को पहली बार न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अपनी असहमति में प्रतिपादित किया था।
1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना के फैसले में बुनियादी संरचना सिद्धांत की जीत हुई। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति निरंकुश थी। हालाँकि, इस ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि हालाँकि संसद के पास “व्यापक” शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके पास संविधान के मूल तत्वों या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने या कमजोर करने की शक्ति नहीं है।
1975 में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने 39वें संशोधन को रद्द करने के लिए बुनियादी संरचना सिद्धांत का इस्तेमाल किया और भारतीय लोकतंत्र की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।
1980 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने के प्रयास में केशवानंद फैसले के जवाब में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम लागू किया गया था। मिनर्वा मिल्स मामले में, नानी पालकीवाला ने 42वें संशोधन की धारा 4 और 55 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सफलतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने मिनर्वा मिल्स फैसले में बताया कि चूंकि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित थी, जैसा कि पहले केशवानंद मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत के माध्यम से माना गया था, संसद संविधान में संशोधन करके इस सीमित शक्ति को परिवर्तित नहीं कर सकती थी। शक्ति को असीमित शक्ति में बदल दिया (जैसा कि 42वें संशोधन द्वारा ऐसा करने का अनुमान लगाया गया था)। इसके अलावा, अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि संसद की “संशोधन करने की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है”।
मूल संरचना सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। यह संसद के सामान्य कृत्यों पर लागू नहीं होता है, जो स्वयं संविधान के अनुरूप होना चाहिए।
केशवानंद में संविधान की “बुनियादी संरचना” में क्या शामिल है, इस पर बहुमत के बीच भी अलग-अलग राय थी।
मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने बहुमत के लिए लिखते हुए संकेत दिया कि मूल संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:
संविधान की सर्वोच्चता.
सरकार का एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप।
संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र.
शक्तियों के पृथक्करण का रखरखाव।
संविधान का संघीय चरित्र.
जस्टिस शेलट और ग्रोवर ने अपनी राय में मुख्य न्यायाधीश की सूची में तीन विशेषताएं जोड़ीं:
एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का अधिदेश राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित है।
भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखना।
देश की संप्रभुता.
जस्टिस हेगड़े और मुखर्जी ने अपनी राय में एक अलग और छोटी सूची प्रदान की:
भारत की संप्रभुता.
राजव्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र.
देश की एकता.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं.
कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश.
न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने यह कहते हुए प्रस्तावना को देखना पसंद किया कि संविधान की बुनियादी विशेषताएं दस्तावेज़ के उस हिस्से द्वारा निर्धारित की गई थीं, और इस प्रकार इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है:
एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य।
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता।
स्थिति और अवसर की समानता.
केशवानंद फैसले के बाद से कई अन्य अदालती फैसलों में मूल संरचना की व्याख्या विकसित हुई है।