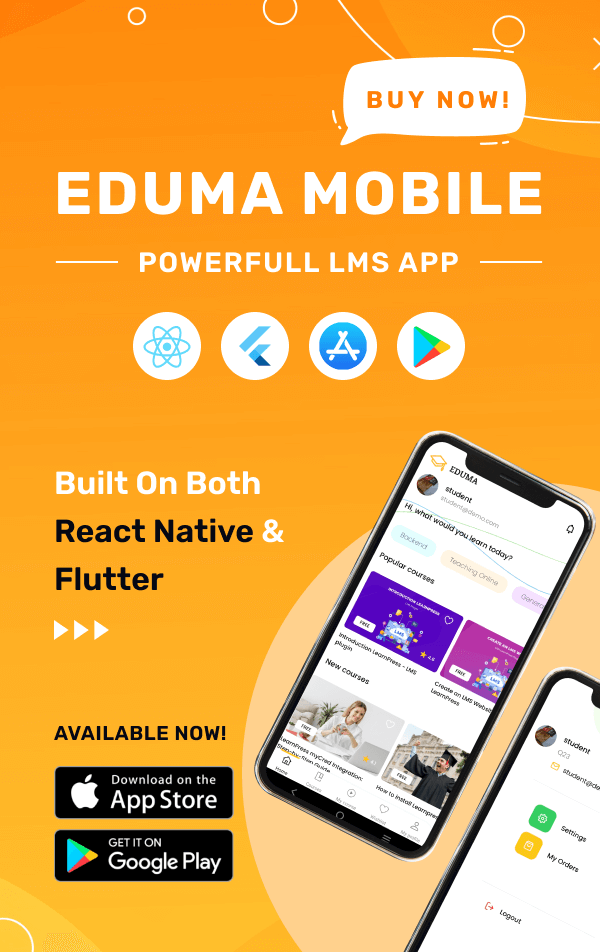यह एक विश्व धर्म है और सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें बुद्ध (शाब्दिक रूप से प्रबुद्ध या जागृत व्यक्ति) के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक थे। तपस्या और ध्यान के बाद, उन्होंने बौद्ध मध्य मार्ग की खोज की – आत्म-भोग और आत्म-पीड़ा की चरम सीमा से दूर संयम का मार्ग। प्रारंभिक ग्रंथों से पता चलता है कि गौतम अपने समय की प्रमुख धार्मिक शिक्षाओं से परिचित नहीं थे, जब तक कि वह अपनी धार्मिक खोज पर नहीं निकल गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मानव स्थिति के लिए अस्तित्व संबंधी चिंता से प्रेरित थे।
सिद्धार्थ का जन्म एक शाही हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन थे, जो शाक्य वंश के नेता थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु, उत्तर प्रदेश थी। उनकी मां रानी माया ने अपने पिता के राज्य जाते समय लुम्बिनी, नेपाल में साल के पेड़ के नीचे एक बगीचे में अपने बेटे को जन्म दिया। शिशु को सिद्धार्थ (पाली: सिद्धार्थ) नाम दिया गया, जिसका अर्थ है “वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है”। जन्म उत्सव के दौरान, साधु द्रष्टा असिता ने अपने पहाड़ी निवास से यात्रा की और घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा (चक्रवर्ती) या एक महान पवित्र व्यक्ति बनेगा।
जब वह 16 वर्ष के हुए, तो उनके पिता ने उनकी शादी चचेरी बहन यशोधरा से कर दी, उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में एक राजकुमार के रूप में 29 साल बिताए थे। हालाँकि उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को वह सब कुछ प्रदान किया जाए जो वह चाहते थे या जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, बौद्ध धर्मग्रंथों में कहा गया है कि भविष्य के बुद्ध ने महसूस किया कि भौतिक धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं था।
29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी प्रजा से मिलने के लिए अपना महल छोड़ दिया। कहा जाता है कि अपने पिता द्वारा बीमार, वृद्ध और पीड़ा को छुपाने की कोशिशों के बावजूद, सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। जब उनके सारथी चन्ना ने उन्हें समझाया कि सभी लोग बूढ़े हो गए हैं, तो राजकुमार महल से आगे की यात्राओं पर चले गए। इन पर उनका सामना एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक सड़ती हुई लाश और एक तपस्वी से हुआ। इसने उन्हें उदास कर दिया, और उन्होंने शुरू में एक तपस्वी का जीवन जीकर उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु पर काबू पाने का प्रयास किया और इसलिए एक भिक्षुक के जीवन के लिए अपना राजसी निवास छोड़ दिया।
गौतम शुरू में राजगृह गए और सड़क पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन शुरू किया। जब राजा बिम्बिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और राजा को उसकी खोज के बारे में पता चला, तो बिमिसार ने सिद्धार्थ को सिंहासन की पेशकश की। सिद्धार्थ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने पर सबसे पहले अपने राज्य मगध का दौरा करने का वादा किया। उन्होंने राजगृह छोड़ दिया और दो साधु शिक्षकों के अधीन अभ्यास किया। अलारा कलामा (स्क्र. अरदा कलामा) की शिक्षाओं में महारत हासिल करने के बाद, उन्हें कलामा ने उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा।
कहा जाता है कि सिद्धार्थ और कौंडिन्य के नेतृत्व में पांच साथियों का एक समूह अपनी तपस्या को और भी आगे ले जाने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने भोजन सहित सांसारिक वस्तुओं के अभाव, आत्म-पीड़ा का अभ्यास करके आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रतिदिन अपने भोजन का सेवन लगभग एक पत्ती या अखरोट तक सीमित करके खुद को लगभग भूखा मरने के बाद, वह नहाते समय एक नदी में गिर गया और लगभग डूब गया। सिद्धार्थ अपने मार्ग पर पुनर्विचार करने लगे। फिर, उसे बचपन का वह क्षण याद आया जिसमें वह अपने पिता को मौसम की जुताई शुरू करते हुए देख रहा था। उन्होंने एकाग्र और एकाग्र अवस्था प्राप्त की जो आनंददायक और ताज़गी देने वाली थी, झाना।
आरंभिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यह महसूस करने के बाद कि ध्यानपूर्ण झन जागृति का सही मार्ग है, लेकिन अत्यधिक तपस्या काम नहीं करती, गौतम ने वह खोजा जिसे बौद्ध मध्य मार्ग कहते हैं – आत्म-भोग की चरम सीमा से दूर संयम का मार्ग। आत्म-पीड़ा.
गौतम प्रसिद्ध रूप से भारत के बोधगया में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे – जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, जब उन्होंने सत्य की खोज होने तक कभी न उठने की कसम खाई थी। कौंडिन्य और चार अन्य साथी यह मानकर चले गए कि उन्होंने अपनी खोज छोड़ दी है और अनुशासनहीन हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 49 दिनों के प्रतिष्ठित ध्यान के बाद, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय से, गौतम को उनके अनुयायी बुद्ध या “जागृत व्यक्ति” के रूप में जानते थे (“बुद्ध” का अनुवाद कभी-कभी “प्रबुद्ध व्यक्ति” के रूप में भी किया जाता है)। उन्हें अक्सर बौद्ध धर्म में शाक्यमुनि बुद्ध, या “शाक्य कबीले के जागृत व्यक्ति” के रूप में जाना जाता है।
बौद्ध धर्म के अनुसार, अपनी जागृति के समय उन्हें दुख के कारण और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कदमों की पूरी जानकारी का एहसास हुआ। इन खोजों को “चार महान सत्य” के रूप में जाना जाता है, जो बौद्ध शिक्षण के केंद्र में हैं। इन सत्यों की महारत के माध्यम से, किसी भी प्राणी के लिए सर्वोच्च मुक्ति या निर्वाण की स्थिति संभव मानी जाती है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की पूर्ण शांति के रूप में वर्णित किया है जो अज्ञानता, लालच, घृणा और अन्य कष्टदायक स्थितियों, या “अपवित्रताओं” (किलेसास) से मुक्त है। निर्वाण को “दुनिया का अंत” भी माना जाता है, इसमें मन की कोई व्यक्तिगत पहचान या सीमाएँ नहीं रहती हैं। ऐसी अवस्था में, कहा जाता है कि एक प्राणी के पास प्रत्येक बुद्ध से संबंधित दस लक्षण होते हैं।
जागृति के बाद, बुद्ध तपुस्सा और भल्लिका नाम के दो व्यापारियों से मिले, जो उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध ने अपने निष्कर्षों को समझाने के लिए असिता और उनके पूर्व शिक्षकों, अलारा कलामा और उद्दाका रामापुत्त से मिलने का इरादा किया था, लेकिन उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने उत्तरी भारत में वाराणसी (बनारस) के पास डियर पार्क की यात्रा की, जहां उन्होंने उन पांच साथियों को अपना पहला उपदेश देकर, जिन्हें बौद्ध लोग धर्म का पहिया कहते हैं, गति प्रदान की, जिनके साथ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके साथ मिलकर, उन्होंने पहला संघ बनाया: बौद्ध भिक्षुओं की कंपनी। सभी पांच अरिहंत बन गए, और पहले दो महीनों के भीतर, यासा और उसके चौवन दोस्तों के धर्म परिवर्तन के साथ, ऐसे अरिहंतों की संख्या 60 हो गई है। इसके बाद कस्पा नाम के तीन भाइयों का धर्म परिवर्तन हुआ, और उनके प्रतिष्ठित 200 हो गए। , क्रमशः 300 और 500 शिष्य। इससे संघ की संख्या 1000 से अधिक हो गई।
कहा जाता है कि अपने जीवन के शेष वर्षों में, बुद्ध ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिणी नेपाल में गंगा के मैदान में यात्रा की और विभिन्न प्रकार के लोगों को शिक्षा दी: कुलीनों से लेकर सड़क पर सफाई करने वाले बहिष्कृत कर्मचारी, अंगुलिमाल जैसे हत्यारे और नरभक्षी तक। जैसे अलावका. शुरू से ही, बौद्ध धर्म सभी जातियों और वर्गों के लिए समान रूप से खुला था, और इसमें कोई जाति संरचना नहीं थी। संघ ने धर्म का प्रचार करते हुए उपमहाद्वीप की यात्रा की। यह पूरे वर्ष जारी रहा, वासना वर्षा ऋतु के चार महीनों को छोड़कर जब सभी धर्मों के तपस्वी शायद ही कभी यात्रा करते थे। एक कारण यह था कि पशु जीवन को नुकसान पहुँचाए बिना ऐसा करना अधिक कठिन था। वर्ष के इस समय में, संघ मठों, सार्वजनिक पार्कों या जंगलों में चले जाते थे, जहाँ लोग उनके पास आते थे।
संघ के गठन के समय पहला वासन वाराणसी में बिताया गया था। इसके बाद, बुद्ध ने राजा बिम्बिसार से मिलने के लिए मगध की राजधानी राजगृह की यात्रा करने का वादा निभाया। इस यात्रा के दौरान, पहले पांच शिष्यों में से एक, अस्साजी द्वारा सारिपुत्त और मौद्गल्यायन को परिवर्तित किया गया, जिसके बाद वे बुद्ध के दो सबसे प्रमुख अनुयायी बन गए। बुद्ध ने अगले तीन सीज़न मगध की राजधानी राजगृह में वेलुवाना बांस ग्रोव मठ में बिताए।
अपने बेटे के जागने की खबर सुनकर, राजा शुद्धोदन ने कुछ समय बाद दस प्रतिनिधिमंडल भेजे और उन्हें कपिलवस्तु लौटने के लिए कहा। पहले नौ अवसरों पर, प्रतिनिधि संदेश देने में विफल रहे, और इसके बजाय अरिहंत बनने के लिए संघ में शामिल हो गए। हालाँकि, गौतम के बचपन के दोस्त (जो अरिहंत भी बन गए) कालूदायी के नेतृत्व में दसवें प्रतिनिधिमंडल ने संदेश दिया।
अपने जागरण के दो साल बाद, बुद्ध वापस लौटने के लिए सहमत हो गए, और कपिलवस्तु तक पैदल दो महीने की यात्रा की, और जाते समय धर्म की शिक्षा दी। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि राजा शुद्धोदन ने संघ को भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया, उसके बाद धर्म वार्ता हुई। कहा जाता है कि इसके बाद वह सोतापन्ना बन गये। यात्रा के दौरान, शाही परिवार के कई सदस्य संघ में शामिल हुए। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद और अनुरुद्ध उनके पांच प्रमुख शिष्यों में से दो बन गए। सात साल की उम्र में उनका बेटा राहुल भी शामिल हो गया और उनके दस प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया। उनके सौतेले भाई नंदा भी शामिल हो गए और अरिहंत बन गए।
माना जाता है कि बुद्ध के शिष्यों में सारिपुत्त, मौद्गल्यायन, महाकश्यप, आनंद और अनुरुद्ध उनके सबसे करीबी पांच थे। उनके दस प्रमुख शिष्यों को उपालि, सुभोति, राहुला, महाकाक्कन और पुन्ना के पंचक द्वारा प्रतिष्ठित रूप से पूरा किया गया था। पांचवें वासन में, बुद्ध वेसाली के पास महावन में रह रहे थे जब उन्होंने अपने पिता की आसन्न मृत्यु की खबर सुनी। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा शुद्धोदन के पास गए और धर्म की शिक्षा दी, जिसके बाद उनके पिता अरिहंत बन गए।
राजा की मृत्यु और दाह संस्कार ननों के एक समूह के निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए था। बौद्ध ग्रंथों में दर्ज है कि बुद्ध महिलाओं को दीक्षा देने के अनिच्छुक थे। उदाहरण के लिए, उनकी पालक माँ महा प्रजापति ने उनसे संपर्क किया और संघ में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हालाँकि, महा प्रजापति जागृति के मार्ग पर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने शाही शाक्य और कोलियान महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व किया, जो राजगृह की लंबी यात्रा पर संघ का अनुसरण कर रहे थे। समय के साथ, जब आनंद ने उनके मुद्दे का समर्थन किया, तो कहा जाता है कि बुद्ध ने पुनर्विचार किया और, संघ के गठन के पांच साल बाद, महिलाओं को नन के रूप में नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों और महिलाओं में जागृति की क्षमता समान होती है। लेकिन उन्होंने महिलाओं को पालन करने के लिए अतिरिक्त नियम (विनय) दिए।
बुद्ध को मगध के शासक सम्राट बिम्बिसार का संरक्षण मिला। सम्राट ने बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार किया और कई बौद्ध “विहारों” की स्थापना की अनुमति दी। इससे अंततः पूरे क्षेत्र का नाम बदलकर बिहार कर दिया गया।
मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के समय अपने चरम पर पहुंच गया था, जिन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने बौद्ध सम्राट के अधीन स्थिरता की एक लंबी अवधि की शुरुआत की। साम्राज्य की शक्ति विशाल थी – बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजदूतों को दूसरे देशों में भेजा जाता था। बुद्ध ने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की और अपने अनुयायियों से व्यक्तिगत मुक्ति के लिए काम करने को कहा। बुद्ध की शिक्षाएँ केवल मौखिक परंपराओं में मौजूद थीं। बौद्ध सिद्धांत और व्यवहार के मामलों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए संघ ने कई बौद्ध परिषदें आयोजित कीं। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के आधुनिक कुशीनगर के कुशीनारा के परित्यक्त जंगलों में परिनिर्वाण प्राप्त किया।