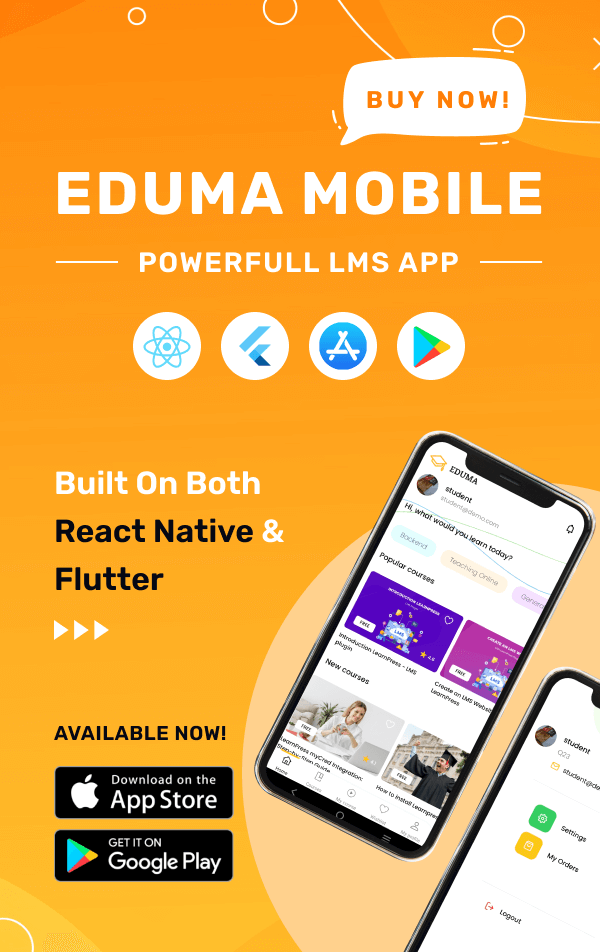भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारतीय रेलवे भारत के आर्थिक विकास में योगदान देता है, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत और मुख्य क्षेत्र की माल ढुलाई आवश्यकताओं की रीढ़ है। यह संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का छह प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से और अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूप से अपने आश्रित संगठनों के माध्यम से देता है।
सड़क परिवहन भारत में परिवहन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। यह देश के हर उस कोने को कवर करता है जिसे रेलवे परिवहन भी कवर नहीं कर पाता। सड़क परिवहन देश के कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है।
बंदरगाहों के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ हैं:
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है – वे भीतरी इलाकों से विदेशों तक महत्वपूर्ण लिंक हैं। वे भीतरी इलाकों से माल की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात और आयात दोनों) बढ़ाते हैं।
- शहरों का विकास – विश्व के अधिकांश प्रमुख शहर बंदरगाह शहर हैं। बंदरगाह अपने आसपास बैंकिंग, वित्त, बीमा, लॉजिस्टिक आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
- रोजगार में वृद्धि-बंदरगाह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष रोजगार से तात्पर्य बंदरगाह संबंधी गतिविधियों में रोजगार से है। बढ़ते औद्योगीकरण और बैंकिंग और बीमा जैसी अन्य सेवाओं में वृद्धि के कारण अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ता है।
- अपेक्षाकृत पर्यावरण के अनुकूल – अन्य परिवहन प्रणालियों की तुलना में, रेलवे परिवहन के लिए दोगुनी ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है, जबकि सड़क परिवहन के लिए समुद्री परिवहन की तुलना में दस गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- विश्व आर्थिक एकीकरण में वृद्धि – बंदरगाहों द्वारा सस्ते परिवहन की सुविधा के कारण वैश्वीकरण आंशिक रूप से सफल रहा है।
- बुनियादी ढांचे का विकास – भीतरी इलाकों और बंदरगाहों के बीच आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से रेलवे, सड़कों और अंतर्देशीय जलमार्गों सहित बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
भारतीय रेल
भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है जिसमें माल ढुलाई, यात्री, पर्यटक, उपनगरीय रेल प्रणाली, टॉय ट्रेन और लक्जरी ट्रेनें शामिल हैं। आईआर में 4,337 ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन हैं, जो ब्रॉड, मीटर और नैरो गेज के मल्टी-गेज नेटवर्क पर संचालित होते हैं। भारतीय रेलवे को 16 जोनों में विभाजित किया गया है और लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन शामिल हैं।
परियोजना योजना एवं कार्यान्वयन
भारतीय रेलवे ने 2012-13 में 1,008 मिलियन टन प्रारंभिक लोडिंग हासिल करके माल लदान में बिलियन क्लब में प्रवेश किया। 2014-15 के लिए निर्धारित लोडिंग लक्ष्य 1,105 मिलियन टन है जो 2013-14 की उपलब्धि से 4.9% अधिक है। बारहवीं योजना में योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) में माल लदान का अनुमान 1,405 मिलियन टन है।
भारतीय रेलवे ने 2013-14 में 8,425.6 मिलियन यात्रियों को ढोया, जो दुनिया की कुल आबादी से लगभग 1,430 मिलियन अधिक है। 2014-15 में यात्री यातायात का वार्षिक लक्ष्य 8,645 मिलियन है, जो 2013-14 की तुलना में 2.6% अधिक है। बारहवीं योजना का लक्ष्य योजना के अंतिम वर्ष में 11,710 मिलियन यात्रियों का है।
चुनौतियाँ
जैसे-जैसे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, बढ़ते यातायात के परिवहन में लाइन और टर्मिनल क्षमता की बाधाओं के कारण आईआर के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसलिए, नेटवर्क, विशेष रूप से एचडीएन मार्गों और इसके फीडर और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है
लंबित परियोजनाओं की एक बड़ी शेल्फ है जिसकी अनुमानित लागत रु। मूल रूप से अनुमानित लागत के आधार पर 4,91,510 करोड़ इनमें से प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे दोहरीकरण, नई लाइनें, गेज परिवर्तन, यातायात सुविधाएं, सिग्नल और दूरसंचार कार्य, कार्यशालाएं और विद्युतीकरण के लिए फंड की आवश्यकता 2,08,054 करोड़ रुपये अनुमानित है।
बजट 2017
5 वर्षों की अवधि में 100,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
- आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए गए रेल टिकटों पर सर्विस चार्ज वापस ले लिया जाएगा.
- लिफ्ट और एस्केलेटर उपलब्ध कराकर 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- तीर्थयात्रा और पर्यटन के लिए समर्पित ट्रेनें शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे
- नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी+. इससे युवाओं के लिए नई नौकरियाँ खुलने की उम्मीद है
- 2017-18 के दौरान कम से कम 25 ट्रेन स्टेशनों को पुरस्कार मिलने की उम्मीद है
- 2019 तक भारतीय रेलवे के सभी कोचों में बायो-टॉयलेट लगा दिए जाएंगे
रेलवे साझेदारी के माध्यम से चयनित वस्तुओं के लिए शुरू से अंत तक परिवहन समाधान को एकीकृत करेगा
2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को ख़त्म किया जाएगा
रेल बजट में 22 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई
आईआर के वित्त की संरचना:
आईआर के वित्त की संरचना ऐसी है कि उन्हें राजस्व और पूंजीगत व्यय में विभाजित किया गया है। जबकि राजस्व व्यय दिन-प्रतिदिन और परिचालन कामकाजी खर्चों का ख्याल रखता है, जिसमें ऋण सेवा और लाभांश भुगतान शामिल है, पूंजीगत व्यय मरम्मत सहित आईआर के निवेश का ख्याल रखता है। और नवीनीकरण. ऐसी तीन धाराएँ हैं जिनमें पूंजीगत व्यय शामिल है; ये वित्त मंत्रालय से सकल बजटीय सहायता, संसाधनों की आंतरिक पीढ़ी और आईआरएफसी से पट्टे हैं।
भारतीय सड़कें
परिचय
भारत के पास 4.7 मिलियन किमी का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यह सड़क नेटवर्क देश के सभी सामानों का 60 प्रतिशत से अधिक और भारत के कुल यात्री यातायात का 85 प्रतिशत परिवहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में शहरों, कस्बों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के साथ सड़क परिवहन धीरे-धीरे बढ़ा है।
प्रमुख निवेश/विकास
1.राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम (NHIDCL) को 2024 तक जम्मू और कश्मीर में 23,000 करोड़ रुपये (3.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की पांच सभी मौसम पहुंच सुरंगों के निर्माण का ठेका दिया गया है।
2.स्पेनिश इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, एबर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर एसए, भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैक्वेरी ग्रुप से 1,000 करोड़ रुपये (150 मिलियन अमेरिकी डॉलर) में दक्षिण भारत में परिचालन में दो टोल रोड परिसंपत्तियां खरीदने पर सहमत हुई है।
भारत के बंदरगाह
परिचय
नौ तटीय भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भारत के सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों का घर हैं। भारत की लंबी तटरेखा भूमि के सबसे बड़े टुकड़े को पानी के भंडार में से एक बनाती है, ये बारह प्रमुख भारतीय बंदरगाह बड़ी मात्रा में कार्गो यातायात और कंटेनर यातायात को संभालते हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 सरकारी हैं और एक, चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह कॉर्पोरेट है। एन्नोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जो काकीनाडा बंदरगाह और निजी कृष्णापटनम बंदरगाह और मुंद्रा बंदरगाह के साथ तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है।
प्रमुख नीति विकास
1:समर्थन प्रदान करने वाली परियोजनाओं में 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है
जल परिवहन की सेवाएँ
2: बंदरगाहों और बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वचालित मंजूरी। हालाँकि, 15 अरब रुपये से अधिक के निवेश के लिए प्रस्ताव को FIPB के पास भेजा जाना आवश्यक है।
3: बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी
4: प्रमुख बंदरगाहों और विदेशी बंदरगाहों, प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों और कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम के गठन की अनुमति दी गई
चुनौतियाँ:
भौगोलिक: भारी गाद जैसा कि हल्दिया जैसे नदी तटीय बंदरगाहों में देखा जाता है।
तकनीकी: अपर्याप्त ड्रेजिंग क्षमताएँ। पारादीप बंदरगाह में खराब मशीनीकरण और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मैन्युअल संचालन
ढांचागत: बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कों की भीड़भाड़ के कारण समय की देरी होती है, जैसा कि जेएलएन बंदरगाह में देखा गया है। बंदरगाहों के भौतिक बुनियादी ढांचे का कम उपयोग, उदाहरण के लिए कोचीन बंदरगाह में।
नीति और नियामक मुद्दे: वर्तमान में बंदरगाह “ट्रस्ट मॉडल” पर काम करते हैं जहां सरकार बंदरगाह की मालिक और ऑपरेटर है। गैर-समान टैरिफ संरचना (टीएएमपी) जो कुछ बंदरगाहों को अप्रतिस्पर्धी बनाती है, बोझिल दस्तावेज़ीकरण और निकासी के कारण अन्य विकसित बंदरगाहों में 6-7 घंटे के औसत समय की तुलना में उच्च टर्नअराउंड समय 3-4 दिन है।