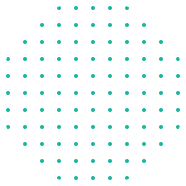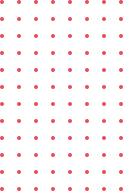Currently Empty: ₹0.00
History
ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प का पतन
ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प का पतन
भारत की पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता “कृषि और हस्तशिल्प का मिश्रण” थी। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इस आंतरिक संतुलन को ब्रिटिश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ख़त्म कर दिया था। इस प्रक्रिया में, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग अपने प्रभुत्व से दूर चला गया और इसका पतन 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक तेजी से जारी रहा। इस प्रक्रिया को ‘डी-औद्योगिकीकरण’ के रूप में जाना जाता है – यह औद्योगीकरण के विपरीत शब्द है। ‘डी-औद्योगिकीकरण’ शब्द का प्रयोग 1940 में हुआ था। इसका शब्दकोश अर्थ है ‘किसी देश की औद्योगिक क्षमता में कमी या विनाश’। यह शब्द भारत में ‘उन्नीसवीं सदी के दौरान ब्रिटिश निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश की प्रक्रिया’ का वर्णन करने के लिए प्रमुखता से आया।
औद्योगीकरण राष्ट्रीय आय के अनुपात में सापेक्ष बदलाव के साथ-साथ कृषि से दूर कार्यबल से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, औद्योगीकरण की प्रगति के साथ, उत्पन्न आय का अनुपात और उद्योग पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत कम होना चाहिए। विनिर्मित वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन के वितरण का अनुमान लगाते हुए, पी. बैरोच ने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 1.9.7 प्रतिशत तक थी। 1800 में। 60 वर्षों की अवधि में, यह गिरकर 8.6 प्रतिशत हो गया। (1860 में) और 1.4 तक। पी.सी. 1913 में। विश्व उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन की घटती हिस्सेदारी को प्रति व्यक्ति विनिर्माण उत्पादन में पूर्ण गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
गिरावट के कारण:
भारतीय अदालतों का पतन: भारतीय अदालतों के लुप्त होने से भारतीय हस्तशिल्प पर पहला झटका लगा। जैसे ही देशी राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए, दरबारों और अन्य औपचारिक अवसरों पर प्रदर्शन के लिए बढ़िया वस्तुओं की मांग गायब हो गई। सामान्य मांग कुछ समय तक जारी रही, लेकिन युवा पीढ़ी के पास कला और हस्तशिल्प को संरक्षण देने के लिए साधन और प्रेरणा का अभाव था। और उन्होंने मना कर दिया.
ब्रिटिश शासन की स्थापना: भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने कुटीर उद्योगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। इससे सीधे तौर पर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसने हथियारों, हथियारों और ढालों की जड़ाई जैसे हस्तशिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यह शिल्प पंजाब और सिंध में आम था। ऐसे हथियारों की आवश्यकता को समाप्त करके और उनके कब्जे और उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, अंग्रेजों ने उद्योग को यूरोपीय पर्यटकों के लिए सजावटी सामान बनाने तक सीमित कर दिया। इसी प्रकार, ब्रिटिश शासन की स्थापना ने, एक अलिखित आदेश के माध्यम से, भारतीयों के लिए ब्रिटिश वरिष्ठों की उपस्थिति में पेटेंट चमड़े के जूते पहनना आवश्यक बना दिया। इससे कढ़ाई वाले जूता उद्योग का पतन हो गया। परोक्ष रूप से, ब्रिटिश शासन ने गिल्डों की शक्ति को खत्म कर दिया जो व्यापार को नियंत्रित करते थे और किए गए काम की गुणवत्ता की निगरानी करते थे। परिणामस्वरूप, कच्चे माल में मिलावट और ख़राब कारीगरी जैसी बुराइयाँ सामने आईं और उत्पादों का कलात्मक और वाणिज्यिक मूल्य ख़राब हो गया।
पश्चिमी शिक्षा: अंग्रेजी शिक्षा की नई प्रणाली एक अन्य सहायक कारक थी। शुरुआती दौर में, नवशिक्षित भारतीय स्वयं यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक पश्चिमीकृत थे। उन्होंने आँख मूँद कर यूरोपीय मानकों और फैशन को स्वीकार कर लिया और हर भारतीय चीज़ को हेय दृष्टि से देखा। मामला इतना ख़राब हो गया कि यूरोपीय रुचियों का अनुसरण करना ही आत्मज्ञान की पहचान माना जाने लगा। परिणामस्वरूप, स्वदेशी उद्योगों के उत्पादों की मांग घट गई जबकि यूरोपीय वस्तुओं की मांग बढ़ गई।
नए पैटर्न का परिचय: भारतीय राज्यों के लुप्त होने के साथ, पुराने शासक और रईस भी गायब हो गए और उनका स्थान यूरोपीय अधिकारियों और पर्यटकों ने ले लिया। हालाँकि, भारतीय कारीगर उन रूपों और पैटर्न को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए जो यूरोपीय रुचि के अनुकूल थे। उन्होंने अपने फॉर्म और पैटर्न की नकल करके अपने नए ग्राहकों को खुश करने की कोशिश की। बहुत बार, नए उत्पाद मूल की बहुत खराब प्रतियां होते थे और उनमें स्वदेशी उत्पादों की “शक्ति और जीवन की कमी” होती थी। इस प्रकार का एक उदाहरण पंजाब में कफ्तागिरी उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो अंधाधुंध यूरोपीय संरक्षण के कारण गिरावट आई थी।
मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा: भारतीय अदालतों के उन्मूलन और विदेशी प्रभावों की शुरूआत के अलावा, यह शक्ति और बेहतर मशीनरी पर आधारित बेहतर विनिर्माण तकनीक थी जिसने ब्रिटिश निर्माताओं को भारतीय कारीगरों को उनके घरेलू बाजार से बाहर निकालने में सक्षम बनाया। इसे रानाडे ‘मनुष्य के श्रम के विरुद्ध प्रकृति की शक्तियों की प्रतिस्पर्धा’ कहते हैं, जिसने भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया। यूरोप में पावरलूम के आविष्कार ने भारतीय कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया और 1834-35 तक, “कपास बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानी इलाकों को ब्लीच कर रही थीं।” यही कहानी अन्य भारतीय उद्योगों जैसे जहाज निर्माण, लोहा गलाने, कांच, रंगाई और कागज निर्माण की भी दोहराई जा सकती है। भारतीय घरेलू और कुटीर हस्तशिल्प संभवतः विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके, जिसे एक शक्तिशाली औद्योगिक संगठन, बड़ी मशीनरी, बड़े पैमाने पर उत्पादन और श्रम के जटिल विभाजन का समर्थन प्राप्त था। स्वेज़ नहर के निर्माण, माल ढुलाई दरों में गिरावट और परिवहन लागत में कमी से भारतीय उद्योगों की कठिनाइयाँ और बढ़ गईं, जिससे ब्रिटिश सामान भारत में और अधिक सस्ता हो गया।
ब्रिटिश सरकार की नीति: शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक हितों ने उसे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि भारत से उसका निर्यात काफी हद तक उन्हीं से होता था। हालाँकि, इस नीति को इंग्लैंड में निहित स्वार्थों के दृढ़ विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने कंपनी को केवल कच्चे माल के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जो कि ब्रिटिश उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक था। भारत को ग्रेट ब्रिटेन के उद्योगों के अधीन बनाने की इस नीति का दुर्लभ दृढ़ संकल्प और घातक सफलता के साथ पालन किया गया। भारतीय कारीगरों, विशेषकर रेशम-वाइंडर्स को कंपनी के कारखानों में काम करने के लिए मजबूर करने के आदेश जारी किए गए, न कि उनके घरों में; वाणिज्यिक निवासियों को भारतीय बुनकरों के गांवों और समुदायों पर व्यापक कानूनी शक्तियां प्रदान की गईं। रंगे हुए भारतीय केलिको का उपयोग निषिद्ध था। भारतीय उद्योगों को कुचलने के लिए सीमा शुल्क का व्यापक उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए, 1813 में, भारत के कपास और रेशम के सामान को ब्रिटिश बाजार में इंग्लैंड में निर्मित कपड़े की कीमत से 50-60% कम कीमत पर लाभप्रद रूप से बेचा जा सकता था। हालाँकि, ब्रिटिश बाज़ार से बाहर निकालने के लिए भारतीय वस्त्रों पर उनके मूल्य पर 70-80% तक शुल्क लगाया गया था।
बिचौलियों की भूमिका: गाँव के निर्वाह और ग्रामीण कला उद्योगों को छोड़कर, अन्य सभी में, बाजार के विस्तार के कारण डीलरों और फाइनेंसरों का उदय हुआ, जिन्होंने कारीगरों को अपने मालिकों के लिए “लकड़ी काटने वाले और पानी निकालने वाले” तक सीमित कर दिया। इस गतिरोध को दूर करने में बिचौलियों द्वारा निभाई गई भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से ही सबसे अच्छी तरह स्पष्ट होती है। कंपनी, कुटीर उद्योगों के उत्पादों की डीलर होने के नाते, तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए नकद और कच्चे माल के रूप में अग्रिम भुगतान करती थी। एक बार ऐसा करने के बाद, इसने कारीगरों को अपनी लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। उदाहरण के लिए, इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक बुनकर, जिसने कंपनी से अग्रिम राशि प्राप्त की थी, वह कपड़ा बेचने पर, “कंपनी को लगे श्रम या उपज को किसी भी कीमत पर किसी अन्य व्यक्ति, यूरोपीय या मूल निवासी को नहीं देगा”। दूसरों के लिए, “बुनकर दीवानी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा”; वह बुनकर “कपड़े के प्रत्येक टुकड़े की निर्धारित कीमत पर 35% जुर्माने के अधीन होगा जिसे वह लिखित समझौते के अनुसार वितरित करने में विफल रहता है”। जब भी कारीगर उन पर थोपे गए समझौतों को पूरा करने में असमर्थ होते थे, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनका सामान जबरन जब्त कर लिया जाता था और मौके पर ही बेच दिया जाता था। इस अन्याय का विरोध करने में असमर्थ, कई बुनकरों ने “रेशम बुनने के लिए मजबूर होने से बचने के लिए अपने अंगूठे काट दिए।”
हस्तशिल्प उद्योग की गिरावट का भारत पर प्रभाव
1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति देने के बाद भारतीय बाजार में सस्ते और मशीन-निर्मित आयात की बाढ़ आ गई। दूसरी ओर, भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अधिक कठिन हो गया। 1820 के बाद, यूरोपीय बाज़ार भारतीय निर्यात के लिए लगभग बंद हो गए। नए शुरू किए गए रेल नेटवर्क ने यूरोपीय उत्पादों को देश के सुदूर कोनों तक पहुंचने में मदद की।
पारंपरिक आजीविका का नुकसान भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ नहीं हुआ, जैसा कि उस समय के अन्य तेजी से औद्योगीकरण वाले देशों में हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उस समय भारत का गैर-औद्योगीकरण हुआ जब यूरोप में फिर से तीव्र औद्योगिक क्रांति देखी जा रही थी। यह ऐसे समय में हुआ जब भारतीय कारीगर और हस्तशिल्पी पहले से ही राजकुमारों और कुलीनों द्वारा संरक्षण खोने के कारण संकट महसूस कर रहे थे, जो अब नए पश्चिमी स्वाद और मूल्यों के प्रभाव में थे। विऔद्योगीकरण की एक अन्य विशेषता कई शहरों का पतन और भारत के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया थी। कई कारीगरों को, कम रिटर्न और दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा (बंगाल में, कंपनी के शासन के दौरान, कारीगरों को कम मजदूरी दी जाती थी और अपने उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था), उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया, गांवों में चले गए और कृषि में लग गए।
इसके परिणामस्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अत्यधिक बोझ वाला कृषि क्षेत्र गरीबी का एक प्रमुख कारण था और इससे गाँव की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। शुद्ध निर्यातक से भारत शुद्ध आयातक बन गया।
विऔद्योगीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन
राष्ट्रवादी और उनकी आलोचना
राष्ट्रवादी, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और आर.सी. दत्त, रजनी पाल्मे दत्त आदि ने भारतीय उद्योग के विनाश को उपनिवेशवाद के परिणाम के रूप में देखा और उन्होंने भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के संदर्भ में विऔद्योगीकरण प्रक्रिया पर चर्चा की। 19वीं सदी की शुरुआत में, लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात में कमी आई, जबकि दूसरी ओर, ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के आयात में वृद्धि हो रही थी। 1860 (96 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग) से 1880 (1 अरब 70 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग) और अंततः 1900 (27 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग) की अवधि के बीच ब्रिटेन द्वारा सूती वस्त्रों के आयात में इस गिरावट का पता लगाया जा सकता है। आर.सी. दत्त और अन्य लोगों का तर्क है कि आयात में गिरावट से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विदेशी बाजारों में भारतीय वस्त्रों की मांग कम हो रही थी और बढ़ते निर्यात से संकेत मिलता है कि भारतीय हस्तशिल्प स्वदेशी बाजार से बाहर हो गए थे। यह नीति, जहां तक संभव हो, भारत के निर्माताओं के स्थान पर ब्रिटिश निर्माताओं को लाने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। 1960 के दशक में डेविड मॉरिस डेविड ने राष्ट्रवादियों की धारणाओं और तर्कों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में विऔद्योगीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए अधिक सबूत उपलब्ध नहीं हैं। मॉरिस ने दावा किया कि ब्रिटिश निर्मित कपड़ों ने भारतीय उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि भारतीयों की क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही थी जिसके कारण भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई; इसलिए स्वदेशी उत्पादन को नुकसान पहुंचाए बिना, ब्रिटिश आयात बढ़ाकर कपड़े की मांग पूरी की गई। मॉरिस के जवाब में बिपिन चंद्रा, टोरू मात्सुई और तपन रॉयचौधरी ने तर्क दिया है कि सबूत विऔद्योगीकरण की ओर इशारा करते हैं। अकाल की रिपोर्टों, चश्मदीद गवाहों और यात्रियों के वृत्तांतों, आधिकारिक पूछताछ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारी रिपोर्टों आदि के आधार पर, ये सभी भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के सबसे खराब संभावित प्रभाव की ओर संकेत कर रहे थे। इन विचारकों ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं था।
बुने हुए कपड़े की कीमत बहुत कम थी। 1849 से 1889 के दौरान कपड़े के आयात में 25.5 मिलियन स्टर्लिंग की वृद्धि हुई, जबकि दूसरी ओर, यार्न के आयात में केवल 1.8 मिलियन स्टर्लिंग की वृद्धि हुई। इसलिए, भारतीय बुनकर यार्न की कीमतों में गिरावट से वास्तव में लाभ नहीं उठा सके, जो तुलनात्मक रूप से कम फलदायी थी क्योंकि इससे उनके कपड़े की लागत में ब्रिटिश मशीन-बुने हुए कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक कमी नहीं आई, जो कि एक था। बहुत सस्ता. मॉरिस ने यह भी तर्क दिया कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर आदि से आयात के बावजूद भारतीय लघु उद्योग बच गया क्योंकि भारतीय लघु उद्योग ने अपना बाजार तैयार किया। हालाँकि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि भारतीय उद्योग को किसी भी विनाश का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मॉरिस ने इस सवाल का आंशिक जवाब दिया कि कैसे राष्ट्र के सामने विषमताओं और प्रतिस्पर्धा के आगमन के बावजूद, मशीन सस्ती होने के बावजूद भारतीय लघु-उद्योग जीवित रहा। आयातित वस्तुएं. हालाँकि, वास्तविकता यह है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बुनकरों ने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें जाति-आधारित व्यवसायों से गहरा लगाव था। दूसरा कारण यह था कि उनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं था और कई लोग कर्ज में फंसे हुए थे।
राष्ट्रवादियों को एक आम आलोचना का सामना करना पड़ा कि उनके पास गैर-औद्योगिकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, विशेष रूप से जनगणना द्वारा की गई रिकॉर्डिंग से पहले की अवधि में। हालाँकि बाद में अमिय कुमार बागची जैसे इतिहासकार कुछ सांख्यिकीय साक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। बागची ने 1809-1813 के बीच गंगा के बिहार में फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन द्वारा किए गए सर्वेक्षण और 1901 की जनगणना के आंकड़ों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य दिखाए। बागची के विश्लेषण के अनुसार, 1809-1813 में उद्योगों पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 18.6 था, जो घट गया। बाद के निष्कर्षों में 8.5 प्रतिशत मारिका विकज़ियानी ने बताया कि बुकानन-हैमिल्टन के सर्वेक्षण को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी एकत्र की, जिन्होंने विदेशियों के मकसद के डर से उन्हें गलत जानकारी दी होगी। स्थानीय लोगों को यह भी संदेह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस जानकारी का उपयोग राजस्व बढ़ाने या उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए कर सकती है। विकज़ियानी ने यह भी तर्क दिया कि बुकानन-हैमिल्टन का स्पिनरों का वर्गीकरण बहुत सटीक नहीं था क्योंकि स्पिनर केवल स्पिनिंग के आधार पर अपना समर्थन नहीं कर सकते थे; उनके विचार में स्पिनरों ने पर्याप्त कमाई नहीं की और उन्हें अंशकालिक स्पिनरों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए स्पिनरों का अनुमान ग़लत था. बागची ने जवाब दिया और कहा कि भले ही कताई ने स्पिनरों को पूरी तरह से समर्थन नहीं दिया, लेकिन यह उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है।
बहस का दूसरा पक्ष
1960 के दशक की शुरुआत में डैनियल थॉर्नर ने तर्क दिया कि 1881-1931 की जनगणना से पता चला कि औद्योगिक व्यवसायों में लगी आबादी के अनुपात में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ था। उन्होंने विस्तार से बताया कि पहली नज़र में, जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि कृषि में पुरुष कार्यबल 65% था और 1931 में बढ़कर 72% हो गया। इसी अवधि में उद्योग में उनका अनुपात 1881 में 16% से घटकर 1931 में 9% हो गया। विचारोत्तेजक डी-औद्योगीकरण। हालाँकि, थॉर्नर ने जनगणना श्रेणियों को गलत बताते हुए इस पर सवाल उठाया क्योंकि इसमें कृषि कार्य-बल और सामान्य श्रम-बल के बीच और औद्योगिक कार्य-बल और व्यापार के बीच स्पष्ट अलगाव माना गया था। डेनियल के विचार में, भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में यह कठिन अलगाव संभव नहीं था, जो मौसमी अवधि के दौरान लोगों को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य करता था।
थॉर्नर के मुताबिक, अगर इन श्रेणियों को मिला दिया जाए तो तस्वीर अलग दिखती है। फिर 1881-1931 के बीच प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि में कार्यबल में वृद्धि लगभग 2% रही और उद्योग और व्यापार में गिरावट केवल 3% रही। थॉर्नर ने महिला श्रम के आंकड़ों को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि जनगणना अधिकारी स्वयं उन्हें गलत मानते हैं। इसलिए उनके विचार में, जो कुछ हद तक विवादास्पद है, जनगणना के आंकड़े पर्याप्त डी-औद्योगिकीकरण का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान नहीं करते हैं। बहरहाल, थॉर्नर ने माना कि 1881 से पहले भारत में डी-औद्योगिकीकरण हो चुका था।
तीर्थंकर रॉय और अन्य लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन्होंने विश्लेषण से महिलाओं को बाहर करने पर आपत्ति जताई है। जनगणना अवधि के दौरान महिलाओं की भागीदारी में नाटकीय रूप से गिरावट आई। ऐसा लगता है कि भारतीय सामाजिक संदर्भ में, कई कारीगर परिवारों में महिलाओं ने घरेलू या कृषि कार्य करने के लिए पुरुषों की तुलना में पहले कारीगरी का काम छोड़ दिया। इसलिए उनके डेटा को शामिल करने से व्यावसायिक संरचना में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा जबकि महिलाओं से संबंधित डेटा को शामिल करने से औद्योगिक गतिविधि में लगे लोगों की संख्या में गिरावट दिखाई देगी। हाल के शोध से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों और वस्तुओं ने मशीन-निर्मित वस्तुओं के प्रभाव को अलग-अलग तरीकों से अनुभव किया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कब औपनिवेशिक शासन के अधीन आए। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश-निर्मित वस्तुओं ने पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित किया। तपन रॉयचौधरी जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि पूर्वी भारत के कारीगरों और बुनकरों की स्थिति प्लासी की लड़ाई (1757) के तुरंत बाद खराब होने लगी और 19वीं शताब्दी में उनकी स्थिति और खराब हो गई। यह भी सुझाव दिया गया है कि मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल और पश्चिमी भारत की तुलना में कम नुकसान हुआ।