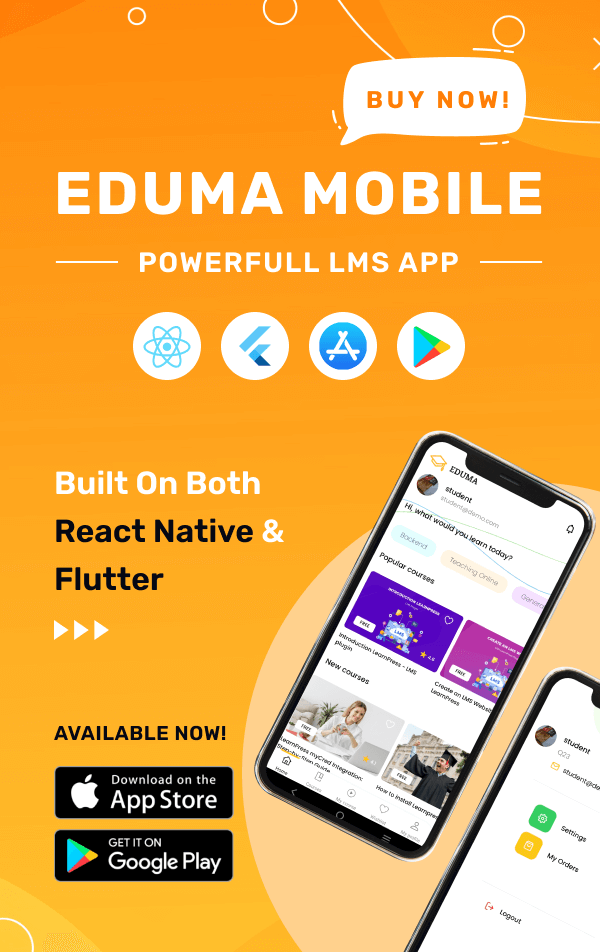1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार किसी प्रकार से ब्रिटिश नियंत्रण में आया। 1854 में, जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को रायपुर में मुख्यालय के साथ एक डिप्टी कमिश्नरशिप के रूप में गठित किया गया। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और राजस्व प्रणालियों में कुछ बदलाव किए, जिसका छत्तीसगढ़ के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की घुसपैठ का बस्तर में आदिवासियों और छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों ने कड़ा विरोध किया और यह 1947 तक जारी रहा।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण:-
निम्नलिखित कारण हैं जिनके कारण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ जैसे:- स्थानीय किसानों का शोषण, इस क्षेत्र में भीषण अकाल का होना, ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण से बचना। पं. द्वारा राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान। सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री माधवराव, श्री मेधावले।
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह ने किया था, जो सोनाखान के दयालु जमींदार थे। वे आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हुए। वीर नारायण सिंह की शहादत को 1980 के दशक में पुनर्जीवित किया गया है और वह छत्तीसगढ़ी गौरव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बस्तर सक्रिय रूप से शामिल था। बस्तर स्वतंत्रता के शुरुआती आंदोलनों में से एक का अभिन्न अंग था।
छत्तीसगढ़ में विद्रोह
आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समृद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने कई आदिवासी विद्रोह देखे हैं। यह अठारहवीं सदी के दौरान शुरू हुआ था और बीसवीं सदी के कुछ दशकों तक जारी रहा। इनमें से कुछ विद्रोहों में स्थानीय जनजातियाँ शामिल थीं लेकिन बाकी बड़े पैमाने पर आंदोलन थे। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं:-
हल्बा विद्रोह – 1774 में शुरू हुआ और 1779 तक जारी रहा
1795 का भोपालपटनम संघर्ष
1825 का परलकोट विद्रोह
तारापुर विद्रोह – 1842 में शुरू होकर 1854 तक जारी रहा
मारिया विद्रोह – 1842 में प्रारंभ होकर 1863 तक जारी रहा
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम – 1856 में प्रारम्भ होकर 1857 तक चला
1859 का कोई विद्रोह
1876 का मुरिया विद्रोह
रानी विद्रोह – 1878 में प्रारम्भ होकर 1882 तक चला
1910 का भूमकाल
कोई विद्रोह
कोई विद्रोह बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जन विद्रोह है। इस विद्रोह का गठन निरंकुश और दबंग ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1859 में हुआ था। आदिवासियों ने अंग्रेजों के उस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें साल के पेड़ों को काटने का ठेका क्षेत्र के बाहर के लोगों को देने की पेशकश की गई थी। बस्तर. हैदराबाद के ठेकेदारों को बस्तर क्षेत्र में साल के पेड़ों को काटने का सौदा पेश किया गया। जमींदारी के लोग, जो पेड़ों की कटाई में शामिल थे, कोइज़ के नाम से जाने जाते थे, जो बाद में क्रांति का नाम बन गया। जिन ठेकेदारों को पेड़ काटने का ठेका दिया गया था, वे निर्दोष आदिवासी लोगों का कई तरह से शोषण करने के लिए भी जाने जाते थे। जब पानी सिर से ऊपर बढ़ गया तो आदिवासियों ने बस्तर में कोई क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वे एक भी पेड़ की कटाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज़ अशांति को दबाना चाहते थे और आदिवासी लोगों के नेतृत्व में विरोध को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार आदिवासी लोग अपने निर्णय पर बहुत दृढ़ थे। वे अपने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध वनों का दोहन नहीं होने देंगे।
मारिया विद्रोह
यह बस्तर क्षेत्र में हुआ था। मारिया जनजाति का विद्रोह एक लम्बा विद्रोह था, जो बीस वर्षों तक चला। मारिया क्रांति बहुत लंबे समय तक चली, वर्ष 1842 से 1863 तक। यह स्पष्ट रूप से मानव बलि की प्रथा को संरक्षित करने के लिए लड़ी गई थी। हालाँकि ऐसे किसी उद्देश्य के लिए लड़ना जिसमें मानव प्रथा की हत्या शामिल हो, बहुत अमानवीय लगता है, लेकिन आदिवासी लोगों के पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मराठों और अंग्रेजों द्वारा सिलसिलेवार आक्रमण हुए। मराठों और अंग्रेजों के संयुक्त शासन ने आदिवासी लोगों के लिए अपनी वैयक्तिकता और मौलिकता को बहाल करना लगभग असंभव बना दिया। एंग्लो-मराठा शासन ने आदिवासी जनजातियों को अपने आदिवासी विश्वासों और प्रथाओं से अलग होने के लिए मजबूर किया। अंग्रेज और मराठा लगातार मंदिरों में प्रवेश करते थे, जिससे आदिवासियों की भोली-भाली मान्यताओं के अनुसार मंदिरों का पवित्र वातावरण प्रदूषित हो जाता था। मारियास की पहचान बचाने का एकमात्र तरीका आक्रमणकारियों के खिलाफ विद्रोह करना था। मारिया विद्रोह को प्रमुख आदिवासी विद्रोहों में से एक माना जाता है।
छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह आंदोलन
मुरिया विद्रोह बस्तर क्षेत्र में प्रकट हुआ एक और विद्रोह है। मुरिया विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1876 में हुई। वर्ष 1867 में गोपीनाथ कपरदास को बस्तर राज्य का दीवान चुना गया। गोपीनाथ कपरदास सीधे-साधे और भोले-भाले आदिवासी लोगों का शोषण करते थे। दीवान के अत्याचारों से निपटने में असमर्थ होने के कारण, आदिवासी लोगों ने राजा से दीवान को पद से हटाने की अपील की लेकिन राजा ने अपनी प्रजा का समर्थन नहीं किया। यह लम्बे समय तक चलता रहा और जब उनकी बार-बार उपेक्षा की जाने लगी तो उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा, विद्रोह का। गुस्से से आगबबूला होकर आदिवासियों ने मुरिया जनक्रांति शुरू कर दी। वर्ष 1876 के 2 मार्च को उग्र आदिवासियों ने राजा के निवास स्थान जगदलपुर को घेर लिया। मुरिया लोगों ने राजा को घेर लिया और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिये। चारों ओर से घिरे राजा को आदिवासी लोगों के बीच उत्पन्न अशांति के बारे में अंग्रेजों को सूचित करने में वास्तविक असुविधा का सामना करना पड़ा। बहुत बाद में, ब्रिटिश सेना भेजी गई जिसने राजा को बचाया और न्याय चाहने वाले आदिवासियों की क्रांति को दबा दिया।
परलकोट विद्रोह
वर्ष 1825 अबूझमारिया लोगों के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष था, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी थे। परलकोट का विद्रोह विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध अबूझमाड़ियों के मन में व्याप्त आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। यह गुस्सा मुख्य रूप से विदेशी शासक मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ था। अबूझमारिया गेंद सिंह ने परलकोट के विद्रोह का नेतृत्व किया और अन्य साथी अबूझमारिया ने उसका समर्थन किया। इस विद्रोह का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया हासिल करना था जो सभी बुराइयों से मुक्त हो। विदेशी फरमान ने मूल जनजातियों की अस्मिता को खतरे में डाल दिया और अबूझमाड़िया इसके खिलाफ खड़े हो गये। मराठों ने स्थानीय लोगों पर भारी कर लगाया, जिसे चुकाना उनके लिए असंभव था। उन्होंने विदेशी शक्तियों द्वारा अपने साथ किये गये अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया। विदेशी घुसपैठ से मुक्त बस्तर बनाने की उनकी इच्छा थी।
तारापुर विद्रोह
तारापुर विद्रोह एक और विद्रोह है जिसमें बस्तर की आम जनता विदेशी शासकों के विरुद्ध खड़ी हुई थी। तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 तक चला। बस्तर के मूल लोगों को लगा कि उनकी स्थानीय परंपरा और संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार, वे अपनी मूल संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए एंग्लो-मराठा शासन के खिलाफ खड़े हुए। जनजातीय लोगों से भारी कर वसूला गया और उन्हें कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। स्थानीय दीवान, जो आम जनता से कर वसूल करते थे, उनके लिए उत्पीड़न का प्रतीक बन गये। सबसे ज़्यादा गुस्सा स्थानीय दीवान पर फूटा क्योंकि उच्च अधिकारी उनकी पहुँच से बाहर थे। आदिवासियों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप तारापुर विद्रोह हुआ।
हल्बा विद्रोह
हल्बा विद्रोह की घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के क्षेत्र में घटित हुई। इसने बस्तर जिले में चिरस्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। चालुक्यों के पतन के बाद स्थितियाँ ऐसी बनीं कि मराठा और अंग्रेज दोनों एक के बाद एक यहाँ शासन करने के लिए आये। वर्ष 1774 में उनके विरुद्ध हल्बा विद्रोह प्रारंभ हुआ। डोंगर के तत्कालीन गवर्नर अजमेर सिंह हल्बा के विद्रोह के सूत्रधार थे। डोंगर में एक नया एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से हल्बा की क्रांति प्रारम्भ हुई। हल्बा जनजाति के साथ-साथ सैनिक भी अजमेर सिंह के साथ खड़े थे। विद्रोह का मुख्य कारण आम लोगों के हाथों में धन और भोजन की कमी थी। लंबे सूखे ने उन लोगों को प्रभावित किया था, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास बहुत कम खेती योग्य भूमि थी। इस गंभीर समस्या के साथ, आम लोगों पर मराठों और अंग्रेजों का दबाव और भय भी था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेनाओं और मराठों ने उनका दमन किया और एक नरसंहार में हल्बा आदिवासी के कई लोग मारे गए। इसके बाद हल्बा की सेना भी हार गई।
स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान
छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह:–
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अलग-अलग समय में सिल्हावा-नगरी, गट्टासिली, रुद्री-नवागांव, महासमुंद, दुर्ग जैसे विभिन्न स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। इन सभी जंगल सत्याग्रहों का इन क्षेत्रों के नेताओं द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया और कई लोगों ने इसमें भाग लिया।
छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन- 1940 के बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत सत्याग्रह पारित किया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा और कई प्रमुख नेताओं ने अलग-अलग स्थानों पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रायपुर पं. रविशंकर शुक्ल को व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया गया और उनके द्वारा इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का सफल नेतृत्व किया गया। इस दौरान सभी प्रमुख नेताओं और अनुयायियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन:-
असहयोग आंदोलन 1920 में गांधीजी द्वारा शुरू किया गया था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत धमतरी से कंडेल नहर आंदोलन के रूप में हुई। इस सिलसिले को सफल बनाने के लिए गांधीजी का पहली बार 1920 में छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। गांधीजी के छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन:-
1930 में जब गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया गया तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से रायपुर में जहां पं. रविशंकर शुक्ल ने इसकी शुरुआत नमक बनाकर की और धमतरी में यह जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ साथ ही गट्टासिली, रुद्री-नवागांव, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर में भी.. इन जगहों पर भी विभिन्न नेताओं ने अवज्ञा की और ब्रिटिश नियमों को तोड़ा। 1931 में गांधी-इरविन समझौते के कारण कुछ समय के लिए इसे रोक दिया गया लेकिन 1932 से फिर यह दूसरी बार शुरू हुआ और 1934 तक जारी रहा।
भारत छोड़ो आंदोलन:-
क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान गांधीजी ने प्रसिद्ध नारा “करो या मरो” दिया। 1942 में जैसे ही गांधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया, इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर भी पड़ा। उसी वर्ष छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में ब्रिटिश सरकार के कार्यों का विरोध करने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व रविशंकर, छेदीलाल सिंह, श्री रघुनंदन सिंगरौल जैसे विभिन्न नेताओं ने किया।
पं. की भूमिका छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में रविशंकर शुक्ल –
पं. रविशंकर शुक्ल का जन्म 1877 में सागर में हुआ और 1907 से वे रायपुर में रहने लगे। 1907 से लेकर अपनी अंतिम सांस 1956 तक उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों में अर्थात होम-रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन, रायपुर कांग्रेस जिला समिति के अध्यक्ष 1920, झंडा-सत्याग्रह के प्रतिनिधि 1923, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में योगदान। वे प्रमुख बने -मप्र मंत्री 1956 में.
एर की भूमिका. छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में राघवेंद्र राव:-
एर. राव छत्तीसगढ़ के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका जन्म 1889 में बिलासपुर में हुआ था और उन्होंने लंदन से उच्च डिग्री हासिल की थी। लंदन से वापस बिलासपुर लौटकर, उन्होंने लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए देश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चल रहे विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 1915 से 1941 तक वे विभिन्न पदों पर निर्वाचित होते रहे।