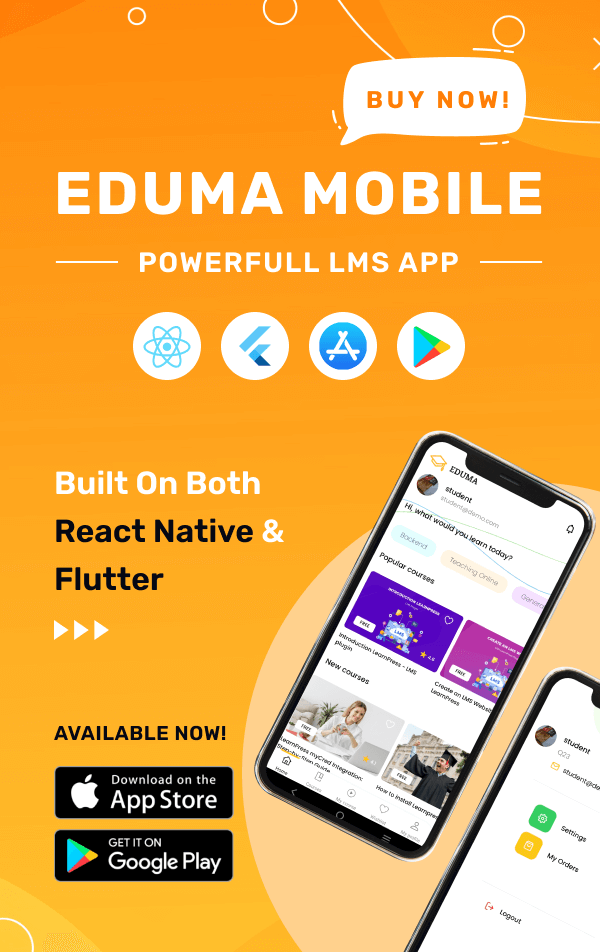प्राकृतिक खतरे गंभीर और चरम मौसम और जलवायु घटनाएं हैं जो दुनिया के सभी हिस्सों में स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं, हालांकि कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में कुछ खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्राकृतिक खतरे तब प्राकृतिक आपदा बन जाते हैं जब लोगों का जीवन और आजीविका नष्ट हो जाती है। छत्तीसगढ़ चक्रवाती तूफान, बाढ़ और सूखे की चपेट में है।
छत्तीसगढ़ में चक्रवात और बाढ़ आपदा
ओडिशा और पूर्वी तटीय क्षेत्र से निकटता के कारण छत्तीसगढ़ चक्रवात और बाढ़ की आपदा के प्रति बहुत संवेदनशील है
चक्रवात हुदहुद: अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हुदहुद एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने पूर्वी भारत में व्यापक क्षति और जानमाल की हानि की। चक्रवाती तूफान हुदहुद के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में तीन दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। यहां तक कि राज्य की राजधानी रायपुर में भी लगातार बारिश हुई।
चक्रवात फेलिन: अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान फेलिन 1999 के ओडिशा चक्रवात के बाद भारत में आने वाला सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का असर तो हुआ, लेकिन जोखिम प्रबंधन की पूर्व योजना काम कर गई और फेलिन राज्य को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सका, जैसी उम्मीद थी.
छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट
सूखा पानी की उपलब्धता में गंभीर कमी को संदर्भित करता है, मुख्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से नहीं, बारिश की कमी के कारण, जिससे कृषि, पेयजल आपूर्ति और उद्योग प्रभावित होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ता है और आबादी के लिए अनकहा दुख ला सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कृषि पर निर्भर हैं और आमतौर पर बंजर भूमि पर रहते हैं। कारण कारक प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं।
छत्तीसगढ़ ने 2015 में 25 जिलों में सूखा घोषित किया। 2016 में फिर से छत्तीसगढ़ की 150 में से 65 से अधिक तहसीलें कम वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति से जूझ रही हैं।
छत्तीसगढ़ में पिछली शताब्दी के दौरान वर्षा परिवर्तनशीलता का अध्ययन 100 वर्षों यानी 1901-2000 के वर्षा आंकड़ों का उपयोग करके किया गया था। वर्षा पैटर्न को समझने के लिए 1900-1950 और 1951-2000 के दौरान औसत वर्षा के बीच अंतर पर काम किया गया था। जीआईएस टूल का उपयोग करके एक जीआईएस मानचित्र तैयार किया गया था और इसे संलग्न चित्र में दिखाया गया है। यह पाया गया कि रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ जैसे कुछ जिलों में वर्षा की मात्रा में कमी आई है, दूसरी ओर वर्षा में कमी आई है। छत्तीसगढ़ ड्राफ्ट के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।
छत्तीसगढ़: प्रारूप प्रबंधन
जोखिम में कमी: राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मिट्टी-नमी संरक्षण उपायों, जल संचयन प्रथाओं, वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने, रिचार्जिंग सहित भूजल क्षमता के विकास और अधिशेष से सतही पानी के हस्तांतरण के माध्यम से सूखे से जुड़ी समस्याओं के प्रति कम संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां संभव और उपयुक्त हों। चारागाह, वानिकी या विकास के अन्य तरीके जिनमें पानी की अपेक्षाकृत कम मांग होती है, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संसाधन विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
दीर्घकालिक हस्तक्षेपों पर दोबारा विचार करना: लोगों को उनके पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल आजीविका चलाने के लिए एक रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम ये हो सकते हैं:
(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तुरंत एक बहु-विषयक टीम गठित करने की आवश्यकता है ताकि विशेष रूप से उन गांवों की पहचान की जा सके जहां मिट्टी और जलवायु स्थितियां ‘पारंपरिक कृषि’ को अस्थिर बनाती हैं।
(ii) ऐसे क्षेत्रों में समुदायों के परामर्श से आजीविका के वैकल्पिक साधन विकसित करने होंगे।
अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन: सहस्राब्दियों से बार-बार सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का अत्यधिक क्षरण हुआ है। ऐसे क्षेत्र देश के कई हिस्सों में पाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली निर्वाह/अस्थायी कृषि उन्हें मामूली सूखे का भी आसान शिकार बना देती है। ऐसे कई अपमानित स्थानों में मानव आबादी ने मुख्य रूप से देहाती अस्तित्व के माध्यम से प्रकृति की अनियमितताओं से निपटने के लिए अपनी जीवन शैली को अनुकूलित किया है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि ऐसी अच्छी तरह से अनुकूलित आबादी ने अधिक लचीलापन और मुकाबला करने की क्षमता विकसित की है। हालाँकि, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि के प्रति गहरा लगाव अक्सर सूखा प्रभावित समुदायों को पारिस्थितिक रूप से अधिक अनुकूल आजीविका की ओर देखने से रोकता है। डीडीपी जैसे कार्यक्रमों ने वैकल्पिक और अधिक टिकाऊ गैर-कृषि आजीविका को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त आजीविका को आगे बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने की रणनीति को ठोस बनाने का मुद्दा आयोग के अधिकार क्षेत्र से परे है; हालाँकि, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर ‘अस्थिर कृषि’ के परिणामस्वरूप होने वाले बार-बार आने वाले संकटों को कम करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन उपायों में उन क्षेत्रों की पहचान करना शामिल हो सकता है जहां पारंपरिक कृषि टिकाऊ नहीं है और ऐसे क्षेत्रों में लोगों को उचित आजीविका व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करने के तरीके तैयार करना आदि शामिल हो सकते हैं।
सरकार. प्राकृतिक आपदा में मकान क्षति के लिए अधिक भुगतान करना
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राकृतिक आपदा में मकानों को हुए नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को संशोधित करने का निर्णय लिया था.
संशोधित दर के अनुसार, प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त पक्के मकान के मालिक को अब 75000 रुपये मिलेंगे। पहले राज्य सरकार 70,000 रुपये का भुगतान कर रही थी। इसी तरह, प्रकृति के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान को 17,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपये का भुगतान किया जाता था।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए अब 12,600 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले राज्य सरकार 6300 रुपये का भुगतान कर रही थी। इसी तरह, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए मुआवजा 3200 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये कर दिया गया है। जिस व्यक्ति की झोपड़ी प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी, उसे अब 2500 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलेंगे।
मानसून के दस्तक देने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है।