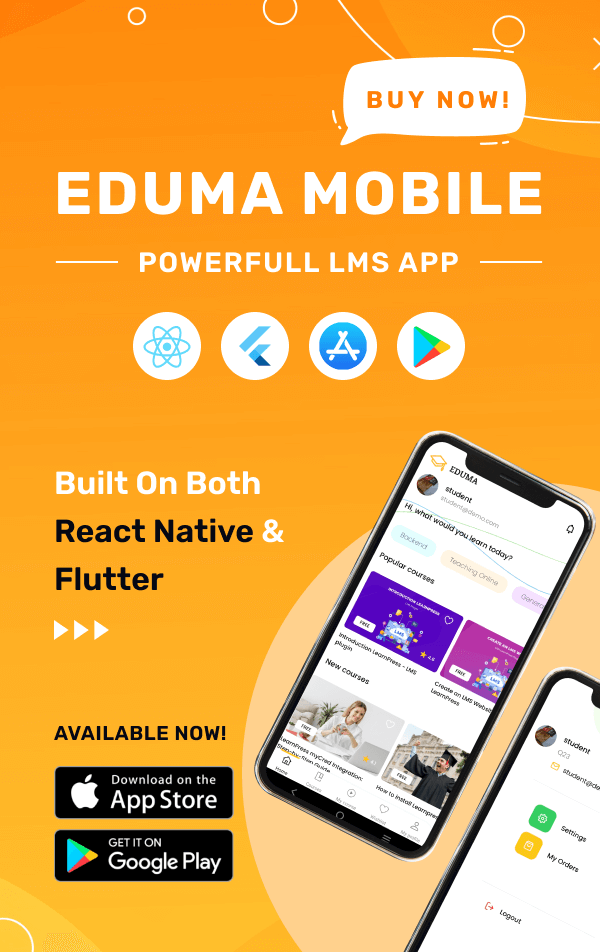छठे देश में ई.पू. उत्तर भारत को सोलह राज्यों में विभाजित किया गया था, जिनमें से अवंती, वत्स, कोशल और मगध अन्य कमजोर राज्यों पर विजय प्राप्त करके प्रमुखता से उभरे। ये चार राज्य आंतरिक झगड़े में शामिल थे, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और राजनीतिक क्षेत्र में महारत हासिल की। भारत का डोमेन.
बिम्बिसार के अधीन मगध:
मगध बिम्बिसार के शासन में प्रमुखता से उभरा, जो हर्यक राजवंश से संबंधित था। संभवतः उसने मगध से बृहद्रथ को उखाड़ फेंका और अपने राज्यारोहण के बाद “श्रीनिक” की उपाधि धारण की। उन्होंने 544 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। से 493 ई.पू. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मगध साम्राज्य की स्थापना थी। साम्राज्य विस्तार के अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उसने चौगुनी नीति अपनाई।
वैवाहिक गठबंधन की नीति:
वैवाहिक गठबंधन की नीति अपनाकर बिम्बिसार ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कोसल के राजा महाकोसल की बेटी कोसलदेवी से विवाह किया, उन्हें दहेज के रूप में काशी गांव मिला, जिससे 1,00,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। “महावंश” में वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बेटी चेल्लाना के साथ उनके विवाह का उल्लेख है।
इसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा में विदेह की राजकुमारी वासवी से विवाह किया। उन्हें मध्य पंजाब के मोदरा के राजा की बेटी खेमा का भी हाथ मिला। इन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना ने मगध साम्राज्य को गौरव प्रदान किया और इसने मगध साम्राज्य और पश्चिम की ओर विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया।
विजय की नीति:
मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए बिम्बिसार की अगली नीति विजय की नीति थी। बिम्बिसार ने अंग राज्य के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया और उसके राजा ब्रह्मदत्त को हराया। अंगा को उसकी राजधानी चंपा के साथ मगध साम्राज्य में मिला लिया गया।
दूर के पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध:
एक दूरदर्शी राजनयिक के रूप में, बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दूर के पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके प्रति मित्रता की नीति अपनाई थी। उन्हें गांधार के शासक पुक्कुसति से एक दूतावास और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ प्रद्योत ने असफल युद्ध किया था। मगध का सबसे दुर्जेय शत्रु अवंती का चंदा प्रद्योत महासेना था जिसने बिंबिसार से युद्ध किया लेकिन अंततः दोनों ने मित्र बनना ही उचित समझा। जब प्रद्योत को पीलिया हो गया तो उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को भी उज्जैन भेजा।
एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण:
प्रशासन की एक अत्यधिक कुशल प्रणाली शुरू करके, बिम्बिसार ने अपनी विजय को मजबूत किया। उनका प्रशासन वास्तव में सुव्यवस्थित और कुशल पाया गया। उच्च अधिकारियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया था, अर्थात्। कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक। सामान्य प्रशासन के प्रबंधन के लिए ‘सबार्थक’ जिम्मेदार थे।
“सेनानायक महामात्र” सैन्य मामलों के प्रभारी थे। “व्यवहारिक महामात्र” न्यायिक-प्रशासन के प्रभारी थे। प्रांतीय प्रशासन भी सुव्यवस्थित था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख “उपराज” होता था। गाँवों को ग्रामीण स्वायत्तता प्राप्त थी। ग्राम प्रशासन का मुखिया “ग्रामिका” होता था। दण्डात्मक कानून कठोर थे। बिम्बिसार ने अच्छी सड़कें बनवाकर संचार के साधन भी विकसित किये। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुरानी राजधानी गिरिव्रज के बाहरी इलाके में स्थित राजगृह में एक नई राजधानी की स्थापना की थी।
उन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को एक सर्वोपरि शक्ति बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में 80,000 गाँव शामिल थे। वह बुद्ध का भी भक्त था। उन्होंने बौद्ध संघ को “बेलुबाना” नामक एक उद्यान दान में दिया। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया था। से 493 ई.पू. उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजातशत्रु था जिसने उसकी हत्या कर दी थी और सिंहासन पर कब्ज़ा कर लिया था।
अजातशत्रु
अजातशत्रु के शासनकाल में बिम्बिसार राजवंश का उत्कर्ष देखा गया। अजातशत्रु ने शुरू से ही विस्तार और विजय की नीति अपनाई। उन्होंने कोसल के प्रसेनजीत के साथ एक लंबा युद्ध शुरू किया, जिसने बिंबिसार को दिए गए काशी गांव के उपहार को रद्द कर दिया था। युद्ध दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग सफलता के साथ कुछ समय तक जारी रहा, जब तक कि प्रसेनजीत ने अपनी बेटी, वजीरा कुमारी की शादी अजातशत्रु से करके और उसे काशी के कब्जे में छोड़कर इसे समाप्त नहीं कर दिया।
अजातशत्रु की अगली उपलब्धि वैशाली के लिच्छवियों की विजय थी। लिच्छवियों के प्रमुख चेतक ने मगध से लड़ने के लिए 36 गणराज्यों को मिलाकर एक मजबूत संघ का गठन किया था। जैन स्रोतों के अनुसार, अपनी मृत्यु से पहले, बिम्बिसार ने अपने हाथी “सेयानागा” “सेचनाका” और दो बड़े रत्नजड़ित हार दिए थे, जिनमें से एक-एक उनके बेटों हल्ला और वेहल्ला को दिया गया था, जो उनकी लिछाहवी मां, चेल्लाना से पैदा हुए थे।
चेतक ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। अपने राज्यारोहण के बाद, अजातशत्रु ने चेतक से उन्हें आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। लेकिन चेतक ने चेतक के सौतेले भाइयों के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। अतः अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच संघर्ष अपरिहार्य हो गया।
बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ गंगा नदी के पास पहाड़ी की तलहटी में एक खदान से निकाले गए रत्नों को उनके बीच बांटने का समझौता किया था। लेकिन लिच्छवियों ने अजातशत्रु को उसके हिस्से से वंचित कर दिया। लेकिन डॉ. एच.सी. रायचौधरी बताते हैं कि युद्ध का सबसे प्रबल कारण मगध के बढ़ते साम्राज्यवाद के खिलाफ गणतांत्रिक राज्यों के बीच आम आंदोलन था।
अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की विस्तृत तैयारी की। संचालन के आधार के रूप में उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पाटलाग्राम में एक किले का निर्माण किया जो अंततः पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध राजधानी के रूप में विकसित हुआ। अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ के सदस्यों के बीच विभाजन पैदा करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने मंत्री वासकारा को नियुक्त किया जिन्होंने सफलतापूर्वक वज्जियन संघ के सदस्यों के बीच मतभेद के बीज बोए और उनकी एकजुटता को तोड़ दिया।
इसके बाद अजातशत्रु ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया और लिच्छवियों को नष्ट करने में उसे पूरे सोलह वर्ष लगे। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मन पर काबू पाने के लिए “महाशिलाकंटक” और “रथमुशला” जैसे कुछ नए हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया। अंततः लिच्छवि को मगध क्षेत्र में मिला लिया गया।
जब अजातशत्रु लिच्छवियों के साथ युद्ध में लगा हुआ था, तब उसे अवंती से खतरे का सामना करना पड़ा। अवंती के राजा चंदा प्रद्योत को उसकी शक्ति से ईर्ष्या होने लगी और उसने मगध पर आक्रमण की धमकी दी। इस खतरे से निपटने के लिए अजातशत्रु ने राजगिरि की किलेबंदी शुरू कर दी। लेकिन उनके जीवन काल में आक्रमण सफल नहीं हुआ।
अजातशत्रु के उत्तराधिकारी:
अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदायिन था जिसने सोलह वर्षों तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथों में उनका वर्णन एक देशद्रोही के रूप में किया गया है, जबकि जैन साहित्य में उनका उल्लेख अपने पिता के प्रति समर्पित पुत्र के रूप में किया गया है। उदयिन ने पाटलिपुत्र शहर को पाटलाग्राम के किले में बनाया, जो पूर्वी भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक राजमार्ग की कमान संभालता था। उसके शासनकाल के दौरान अवंती को मगध के प्रभुत्व से ईर्ष्या होने लगी और दोनों के बीच उत्तरी भारत पर कब्ज़ा करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई।
हालाँकि, उदयिन को अवंती के खिलाफ मगध की अंतिम जीत देखने के लिए जीवित रहना तय नहीं था। जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने पाटलिपुत्र में एक चैत्य का निर्माण कराया। उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार आठवीं और चौदहवीं तिथियों पर उपवास भी रखा। ऐसा कहा जाता है कि उदयिन की हत्या अवंती के राजा पलाका द्वारा किए गए हत्यारे द्वारा की गई थी। सीलोन के इतिहास के अनुसार उदयिन के बाद तीन राजा अनिरुद्ध, मंदा और नागदासका आए।
सीलोनीज़ इतिहास में वर्णन है कि तीनों राजा परजीवी थे। लोगों ने उनके शासन से नाराज़ होकर अंतिम राजा नागदासक के खिलाफ विद्रोह किया और मगध के सिंहासन पर एक अमात्य शिशुनाग को बैठाया। इस पुनर्स्थापना के साथ हर्यक वंश का शासन समाप्त हो गया और सिसुनाग वंश का शासन अस्तित्व में आया।
मगध के सिंहासन पर बैठने से पहले सिसुनाग ने काशी के वाइसराय के रूप में कार्य किया था। उन्होंने गिरिवरजा में अपनी राजधानी स्थापित की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती पर विजय और कब्ज़ा था। इससे मगध और अवंती के बीच सौ साल की प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई। संभवतः उसने वत्स और कोशल राज्यों को मगध में मिला लिया था। अपने पुनरुद्धार के बाद के हिस्से में उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित कर दिया।
सिसुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालासोका या काकवर्ण हुआ। कालासोक का शासनकाल दो घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात्, मगध की राजधानी को गिरिराज से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करना और वैशाली में दूसरी बौद्ध कांग्रेस का आयोजन करना। बहुत दुर्भाग्य से, उन्होंने एक महल क्रांति में अपना जीवन खो दिया, जिसने नंदों को मगध के सिंहासन पर बैठाया। हड़पने वाला शायद नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और उसने संयुक्त रूप से शासन करने वाले कालासोक के दस पुत्रों को भी मार डाला था। इस प्रकार सिसुनाग राजवंश के बाद नंदों का नया राजवंश आया।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना:
मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ई.पू. चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया युद्ध इतिहास की एक अनोखी घटना थी।
विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह 327 ईसा पूर्व के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में सिकंदर के विजयी अभियानों के तुरंत बाद पाया गया था। – 325 ई.पू.
मौर्यों की वंशावली के संबंध में कोई एकमत नहीं है। पुराणों में उनका वर्णन शूद्र और धर्मनिष्ठ के रूप में किया गया है, संभवतः इसका कारण यह है कि मौर्य अधिकतर विधर्मी संप्रदायों के संरक्षक थे।
बौद्ध कार्यों (जैसे महावंश और महावंशतिका) ने मौर्य राजवंश को शाक्य जनजाति से जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे बुद्ध संबंधित थे। दिव्यावदान में चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को क्षत्रिय मुर्दाभिषिक्त अथवा अभिषिक्त क्षत्रिय बताया गया है।
बौद्ध लेखकों के अनुसार, जिस क्षेत्र से मौर्य आए थे वह मोरों (संस्कृत में मयूरा और पाली में मोरा) से भरा हुआ था, और इसलिए उन्हें मोरिया (मौर्य का पाली रूप) के रूप में जाना जाने लगा। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध अशोक तथा उसके पूर्ववर्तियों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयास कर रहे थे।
हेमचंद्र के परिसिष्ठपर्वन में दी गई जैन परंपरा चंद्रगुप्त को मोर-वशीकरण करने वालों (मयुरा-पोशाका) के एक गांव के मुखिया की बेटी के बेटे के रूप में बताती है। विशाखादत्त के मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त के लिए ‘वृषला’ और ‘कुल-हिना’ शब्द के प्रयोग का संभवतः अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त एक अज्ञात परिवार का वंशज मात्र था।
जस्टिन जैसे यूनानी शास्त्रीय लेखक, चंद्रगुप्त मौर्य को विनम्र मूल के व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन उनकी सटीक जाति का उल्लेख नहीं करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख (150 ई.) में वैश्य पुष्यगुप्त को मौर्य राजा चंद्रगुप्त का प्रांतीय गवर्नर बताया गया है। पुष्यगुप्त के चंद्रगुप्त के बहनोई होने का एक संदर्भ है जिसका अर्थ है कि मौर्य वैश्य मूल के रहे होंगे।
निष्कर्ष में, हम कह सकते हैं कि मौर्य तुलनात्मक रूप से विनम्र मूल के थे और मोरिया जनजाति से संबंधित थे और निश्चित रूप से निम्न जाति के थे।
चन्द्रगुप्त मौर्य (321-297 ई.पू.):
चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में नंद सिंहासन पर बैठे। 25 वर्ष की आयु में अंतिम नंद शासक (धनानंद) को गद्दी से हटाने के बाद। वह ब्राह्मण कौटिल्य का आश्रित था, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, जो सिंहासन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने दोनों में उनका मार्गदर्शक और गुरु था।
मगध का अधिग्रहण नए राजवंश की स्थापना में पहला कदम था। एक बार जब गंगा घाटी उनके नियंत्रण में आ गई, तो चंद्रगुप्त सिकंदर के जाने से पैदा हुई शक्ति शून्यता का फायदा उठाने के लिए उत्तर-पश्चिम की ओर चले गए। उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र तेजी से उसके हाथ लगे।
मध्य भारत में वापस आकर उसने नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 305 ई.पू. उसे उत्तर-पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर (अलेक्जेंडर के जनरल जिसने मैसेडोनियन साम्राज्य के अधिकांश एशियाई प्रांतों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था) के खिलाफ एक अभियान में शामिल देखा, जिसे चंद्रगुप्त ने अंततः 303 ईसा पूर्व में जीत लिया था। दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और विवाह गठबंधन में प्रवेश किया।
किसने किसकी बेटी से शादी की यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है? लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त ने ग्रीक जनरल को 500 हाथियों का उपहार दिया और सिंधु के पार का क्षेत्र प्राप्त किया, जैसे पारोपनिसादाई (काबुल), एरिया (हेरात), अराचोइसा (कंधार), और गेड्रोसिया (बलूचिस्तान) के क्षत्रप। सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज कई वर्षों तक पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में रहे और देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की।
जैन स्रोतों (परिसिस्टपर्वन) के अनुसार, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से हट गए। कहा जाता है कि जैन संत भद्रबाहु और कई अन्य भिक्षुओं के साथ वह मैसूर के पास श्रवण बेलगोला गए थे, जहां उन्होंने जानबूझकर स्वीकृत जैन शैली (सल्लेखना) के अनुसार खुद को भूखा रखकर मार डाला।
कौटिल्य और अर्थशास्त्र:
कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उनकी सहायता से चन्द्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखा गया था। यह मौर्यों का इतिहास लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे 15 अधिकरणों या खंडों और 180 प्राकरणों या उपविभागों में विभाजित किया गया है। इसमें लगभग 6,000 श्लोक हैं। इस पुस्तक की खोज शमाशास्त्री ने 1909 में की थी और उन्होंने इसका कुशल अनुवाद किया।
यह शासन कला और लोक प्रशासन पर एक ग्रंथ है। इसकी तिथि और लेखकत्व पर विवाद के बावजूद, इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मौर्य काल की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का स्पष्ट और पद्धतिगत विश्लेषण देता है।
अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त प्रशासनिक शब्दों के बीच समानता निश्चित रूप से यह बताती है कि मौर्य शासक इस कार्य से परिचित थे। इस प्रकार उनका अर्थशास्त्र सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के साथ-साथ मौर्य प्रशासन के संबंध में उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है।
राजा:
कौटिल्य का सुझाव है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए और उसे सारी शक्तियाँ अपने हाथों में केन्द्रित करनी चाहिए। उसे अपने क्षेत्र पर अप्रतिबंधित अधिकार का आनंद लेना चाहिए। लेकिन साथ ही, उसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और अपने मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकार राजा को निरंकुश होते हुए भी अपने अधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए।
वह सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान होना चाहिए। उसे अच्छी तरह से पढ़ा-लिखा भी होना चाहिए ताकि वह अपने प्रशासन के सभी विवरणों को समझ सके। उनका कहना है कि उनके पतन का मुख्य कारण यह है कि राजा का झुकाव बुराई की ओर है। उन्होंने छह बुराइयों की सूची बनाई जिनके कारण राजा का पतन हुआ। वे अहंकार, वासना, क्रोध, लालच, घमंड और सुखों का प्यार हैं। कौटिल्य का कहना है कि राजा को आराम से रहना चाहिए लेकिन उसे भोग-विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए।
राजत्व के आदर्श:
कौटिल्य के अनुसार राजसत्ता का प्रमुख आदर्श यह है कि उसकी अपनी भलाई उसके लोगों की भलाई में निहित है, केवल खुशहाल प्रजा ही अपने संप्रभु की खुशी सुनिश्चित करती है। वह यह भी कहते हैं कि राजा को ‘चक्रवर्ती’ या विभिन्न लोकों का विजेता होना चाहिए और अन्य देशों को जीतकर गौरव प्राप्त करना चाहिए।
उसे अपने लोगों को बाहरी खतरों से बचाना चाहिए और आंतरिक शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। कौटिल्य का कहना था कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले सैनिकों को ‘पवित्र युद्ध’ की भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। उनके अनुसार देशहित में छेड़े गए युद्ध में सब जायज है।
मंत्रियों के बारे में:
कौटिल्य का कहना है कि राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मंत्रियों के बिना राजा एक पहिए वाले रथ के समान है। कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्रियों को बुद्धिमान एवं बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन राजा को उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए.
उन्हें उनकी अनुचित सलाह को त्याग देना चाहिए। मंत्रियों को मिलकर काम करना चाहिए; एक टीम। उन्हें गोपनीयता में बैठकें करनी चाहिए. उनका कहना है कि जो राजा अपने रहस्यों को गुप्त नहीं रख सकता, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता।
प्रांतीय प्रशासन:
कौटिल्य हमें बताते हैं कि राज्य शाही परिवार के सदस्यों द्वारा शासित कई प्रांतों में विभाजित था। सौराष्ट्र और कंभोज आदि जैसे कुछ छोटे प्रांत थे, जिनका प्रशासन ‘राष्ट्रीय’ कहलाने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था जिन्हें फिर से गांवों में विभाजित किया गया था। जिले के मुख्य प्रशासक को ‘स्थानिक’ कहा जाता था जबकि ग्राम प्रधान को ‘गोप’ कहा जाता था।
नागरिक प्रशासन:
बड़े शहरों के साथ-साथ राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन भी बहुत कुशलता से चलाया जाता था। पाटलिपुत्र को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सेक्टर के प्रभारी अधिकारी को ‘स्थानिक’ कहा जाता था। उन्हें कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जिन्हें ‘गोप’ कहा जाता था जो 10 से 40 परिवारों के कल्याण की देखभाल करते थे। पूरे शहर का प्रभार एक अन्य अधिकारी के पास था जिसे ‘नागरिक’ कहा जाता था। नियमित जनगणना की व्यवस्था थी।
जासूसी संगठन:
कौटिल्य का कहना है कि राजा को जासूसों का एक नेटवर्क रखना चाहिए जो उसे देश, प्रांतों, जिलों और कस्बों में होने वाली छोटी-छोटी बातों और घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित करते रहें। गुप्तचरों को अन्य अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए। देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए जासूस होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, महिला जासूस पुरुषों की तुलना में अधिक कुशल होती हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से जासूस के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, राजाओं को राजनीतिक महत्व की जानकारी इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी देशों में अपने एजेंट भेजने चाहिए।
शिपिंग:
एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें कौटिल्य से मिलती है वह मौर्यों के अधीन शिपिंग के बारे में है। प्रत्येक बंदरगाह की निगरानी एक अधिकारी द्वारा की जाती थी जो जहाजों और घाटों पर निगरानी रखता था। व्यापारियों, यात्रियों और मछुआरों पर टोल लगाया गया। लगभग सभी जहाज और नावें राजाओं के स्वामित्व में थीं।
आर्थिक स्थिति:
कौटिल्य का कहना है कि गरीबी विद्रोह का एक प्रमुख कारण है। इसलिए इसे खरीदने के लिए भोजन और धन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह असंतोष पैदा करता है और राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए कौटिल्य राजा को अपनी प्रजा की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने की सलाह देता है। कौटिल्य का कहना है कि गांवों में आय का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था जबकि शहरों में माल की बिक्री पर कर मुख्य स्रोत था।
बिन्दुसार (297-272 ई.पू.):
297 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, जिसे यूनानियों में अमित्रोचेट्स (संस्कृत, अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला) के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार ने दक्कन में अभियान चलाया और प्रायद्वीप में मौर्य नियंत्रण को दक्षिण में मैसूर तक फैलाया।
ऐसा कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों, संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी। हालाँकि, पूर्वी तट पर कलिंग (आधुनिक उड़ीसा) शत्रुतापूर्ण रहा और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने बाद के शासनकाल में उस पर विजय प्राप्त कर ली।
विदेशी मामलों में, बिन्दुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित हेलेनिक पश्चिम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। ऐसा कहा जाता है कि उसका सीरिया के राजा एंटिओकस आई सोटर, सेल्यूकस निकेटर के बेटे, के साथ संपर्क था, जिसके राजदूत डेमाचोस के बारे में कहा जाता है कि वह उसके दरबार में था।
व्यापक रुचियों और रुचियों का एक व्यक्ति, उसने एंटिओकस प्रथम से अनुरोध किया कि वह उसे कुछ मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट भेजे; हालाँकि, अंतिम निर्यात के लिए नहीं था, भेजा नहीं जा सका। प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र के टॉलेमी फिलाडेलपस ने डायोनिसियस को भारत में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। अशोकवदान हमें सूचित करता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जब नागरिकों ने उच्च अधिकारियों के उत्पीड़न पर आपत्ति जताई थी। बिंदुसार ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए अशोक को भेजा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक किया।
अशोक (268-232 ईसा पूर्व):
बिन्दुसार की मृत्यु 272 ई.पू. उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यह चार वर्षों तक चला और 268 ई.पू. अशोक सफल हुए। अशोकवदान के अनुसार, सुभद्रांगी अशोक की मां थीं और यह उन्हें चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी के रूप में वर्णित करता है।
दिव्यावदान संस्करण काफी हद तक अशोकवदान से सहमत है। उसे जनपदकल्याणी, या उसी स्रोत के दूसरे संस्करण में सुभद्रांगी कहा जाता है। सीलोनीज़ स्रोत में, वामसत्थपकासिनी रानी माँ को धर्मा कहा जाता है।
किंवदंती के अनुसार, एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक को उज्जैन के वायसराय का कार्यभार सौंपा गया था। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ऐसा उन्होंने स्थानीय जनता को नाराज किये बिना किया। इसकी पुष्टि तक्षशिला के एक अरामी शिलालेख से की जा सकती है जिसमें वायसराय गवर्नर प्रियदर्शी का उल्लेख है।
उज्जैन के अपने वायसराय काल के दौरान उन्हें विदिसा के एक व्यापारी की बेटी से प्यार हो गया, जिसे देवी या विदिशमहादेवी या शाकयानी कहा जाता है। अशोक की दो अन्य प्रसिद्ध रानियाँ करुवाकी और असंधिमित्रा थीं। दूसरी रानी, करुवाकी का उल्लेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर अंकित रानी के आदेश में किया गया है, जिसमें उनके धार्मिक और धर्मार्थ दान का उल्लेख है। उन्हें अशोक के एकमात्र पुत्र राजकुमार तिवरा की मां के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उल्लेख शिलालेख में उनके नाम से किया गया है।
जहां तक अशोक के सिंहासन पर बैठने का संबंध है, सूत्रों में आम सहमति है कि अशोक युवराज नहीं था बल्कि अपने भाइयों की हत्या के बाद सिंहासन पर बैठा था। हालाँकि, संघर्ष की प्रकृति या उसके भाइयों की संख्या के संबंध में ग्रंथों में कोई एकमत नहीं है।
महावंश में एक जगह कहा गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, जबकि अन्यत्र उसी काम में और दीपवंश में भी कहा गया है कि उसने निन्यानवे भाइयों की हत्या कर दी थी। महावंश में कहा गया है कि यद्यपि उसने निन्यानबे भाइयों को मौत की सजा दी, अशोक ने उनमें से सबसे छोटे, तिस्सा की जान बचाई, जिसे बाद में वाइस-रेजिस्टेंट बनाया गया (वह उपदेशक महाधम्मरक्खिता के प्रभाव में आकर धार्मिक भक्ति के जीवन में सेवानिवृत्त हो गया) और फिर एकविहारिका के नाम से जाना जाता है)। ऐसा लगता है कि हालाँकि संघर्ष हुआ था, लेकिन इसके बहुत से वर्णन सीधे तौर पर अतिशयोक्ति हैं।
तारानाथ के अनुसार, सिंहासन पर बैठने के बाद, अशोक ने कई वर्ष आनंददायक गतिविधियों में बिताए और परिणामस्वरूप उसे कामसोका कहा गया। इसके बाद अत्यधिक दुष्टता का दौर आया, जिससे उसे कैंडासोका का नाम मिला। अंततः उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उसके बाद की धर्मपरायणता के कारण उन्हें धम्मसोक कहा जाने लगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 260 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ विजयी युद्ध के बाद उसका बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना था। कलिंग ने भूमि और समुद्र दोनों द्वारा दक्षिण भारत के मार्गों को नियंत्रित किया, और इसलिए यह आवश्यक था कि वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने।
13वें प्रमुख शिलालेख में इस युद्ध की भयावहता और दुखों तथा इससे अशोक को हुए गहरे पश्चाताप का स्पष्ट वर्णन है। मौर्य सम्राट के शब्दों में, ‘एक लाख पचास हजार लोगों को निर्वासित किया गया, एक लाख लोगों को मार दिया गया और उससे कई गुना अधिक संख्या में लोग मारे गए। अतीत में यह कहा गया है कि युद्ध के तुरंत बाद नाटकीय ढंग से उसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था, इसके साथ-साथ भयावहता के कारण भी।
लेकिन ऐसा नहीं था, और जैसा कि उनके शिलालेखों में से एक, भाबरा शिलालेख में कहा गया है, दो साल से अधिक की अवधि के बाद ही वह एक बौद्ध भिक्षु, उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक बन गए।
उन्होंने बौद्ध पंथ, बुद्ध में आस्था, धम्म (बुद्ध की शिक्षाएं) और संघ के प्रति अपनी स्वीकृति भी बताई है। स्थानीय बौद्ध पादरी के लिए विशेष रूप से लिखा गया, वह खुद को ‘मगध के राजा’ के रूप में भी संदर्भित करता है, एक शीर्षक जिसका उपयोग वह केवल इस अवसर पर करता है।
उनके शासनकाल के दौरान 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की बैठक के साथ बौद्ध चर्च का पुनर्गठन किया गया था। मोगल्लीपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में लेकिन सम्राट ने स्वयं अपने शिलालेखों में इसका उल्लेख नहीं किया है।
यह इस बात पर जोर देता है कि अशोक बौद्ध धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत समर्थन और सम्राट के रूप में किसी भी धर्म के पक्ष में अनासक्त और निष्पक्ष रहने के अपने कर्तव्य के बीच अंतर करने में सावधान था। तीसरी बौद्ध परिषद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बौद्ध संप्रदाय से असंतुष्टों और नवप्रवर्तकों दोनों को बाहर करने के लिए अधिक सांप्रदायिक बौद्धों, थेरवाद स्कूल का अंतिम प्रयास था।
इसके अलावा, इसी परिषद में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में मिशनरियों को भेजने और बौद्ध धर्म को सक्रिय रूप से धर्मांतरण कराने वाला धर्म बनाने का निर्णय लिया गया था।
अशोक ने अपने 13वें प्रमुख शिलालेख में हेलेनिक दुनिया में अपने विभिन्न समकालीनों का उल्लेख किया है जिनके साथ उन्होंने राजनयिक और अन्यथा मिशनों का आदान-प्रदान किया। इनकी पहचान सीरिया के एंटिओकस द्वितीय थियोस, (अम्तियोगा) सेल्यूकस निकेटर के पोते के रूप में की गई है; मिस्र के टॉलेमी III फिलाडेल्फ़स (तुलमाया); मैसेडोनिया के एंटीगोनस गोनाटस (एंटेकिना); साइरेन (माका) के मगस और एपिरस (एलिक्यशुदाला) के अलेक्जेंडर।
बाहरी दुनिया के साथ संचार अब तक अच्छी तरह विकसित हो चुका था। पुरातात्विक आंकड़ों से पुष्ट अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य की सीमा के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं।
मगध मौर्यों का गृह प्रांत था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। शिलालेखों में उल्लिखित अन्य शहरों में आंध्र प्रदेश में उज्जैन, तक्षशिला, भुवनेश्वर के पास तोसाली, कौशांबी और सुवर्णगिरि शामिल हैं।
परंपरा के अनुसार, कश्मीर को अशोकन साम्राज्य में शामिल किया गया था और अशोक ने श्रीनगर शहर का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में खोतान भी मौर्य प्रभाव में आया था।
मौर्यों का आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों से घनिष्ठ संबंध था क्योंकि तलहटी क्षेत्र साम्राज्य का हिस्सा थे। कहा जाता है कि अशोकन की एक बेटी की शादी नेपाल के पहाड़ों के एक कुलीन व्यक्ति से हुई थी।
पूर्व में मौर्यों का प्रभाव गंगा डेल्टा तक फैला हुआ था। ताम्रलिप्ति या आधुनिक तामलुक बंगाल तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से जहाज बर्मा, श्रीलंका के साथ-साथ दक्षिण भारत के लिए रवाना होते थे। पश्चिमी तट पर एक अन्य प्रमुख बंदरगाह नर्मदा के मुहाने पर ब्रोच था।
कंधार ने मौर्य साम्राज्य का सबसे पश्चिमी विस्तार बनाया और अशोक के शिलालेखों में गांधार, कम्बोज और योनास को उसकी सीमाओं के रूप में उल्लेख किया गया है। उत्तर-पश्चिम में मौर्यों ने अपने पड़ोसियों, सेल्यूसिड साम्राज्य और यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा।
श्रीलंका के साथ मौर्य के संबंध बहुत घनिष्ठ थे और अशोक ने अपने पुत्र महिंद्रा और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। दक्षिण में अशोक के शिलालेखों में कई लोगों का उल्लेख है जिनके साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे – चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र (प्रमुख शिलालेख II)।
साम्राज्य का विघटन:
अपने शासनकाल के अंत में अशोक की शाही संगठन पर पकड़ कमजोर हो गई। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। परवर्ती मौर्यों के साक्ष्य बहुत कम हैं।
बौद्ध और जैन साहित्य के अलावा पुराण हमें बाद के मौर्यों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें कोई सहमति नहीं है। पुराणों में भी एक पुराण से दूसरे पुराण में बहुत भिन्नता है। एक कथन जिस पर सभी पुराण सहमत हैं वह यह है कि राजवंश 137 वर्षों तक चला।
अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में विभाजित हो गया। उत्तर-पश्चिमी प्रांत, गांधार और कश्मीर सहित पश्चिमी भाग कुणाल (अशोक के पुत्रों में से एक) द्वारा शासित था और फिर कुछ समय के लिए संप्रति द्वारा शासित था (जैन परंपरा के अनुसार वह अशोक का पोता और जैन धर्म का संरक्षक था)।
बाद में इसे बैक्ट्रियन यूनानियों द्वारा उत्तर-पश्चिम से खतरा पैदा हो गया, जिनके हाथों यह व्यावहारिक रूप से 180 ईसा पूर्व तक खो गया था। दक्षिण से, ख़तरा आंध्रसोरथे सातवाहनों द्वारा उत्पन्न किया गया था जो बाद में दक्कन में सत्ता में आए।
मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भाग, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर दशरथ (संभवतः अशोक के पोते में से एक) का शासन था। मत्स्य पुराण में वर्णित होने के अलावा दशरथ के बारे में हमें नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं से भी पता चलता है, जिन्हें उन्होंने आजीविकों को समर्पित किया था।
पुराणों के अनुसार दशरथ ने आठ वर्षों तक राज्य किया। इससे पता चलता है कि वह सिंहासन पर आने के लिए पर्याप्त उम्र के उत्तराधिकारी के बिना मर गया। वही स्रोत कुणाल के आठ वर्षों तक शासन करने की बात करते हैं।
उनकी मृत्यु भी लगभग उसी समय हुई होगी जब दशरथ की मृत्यु हुई होगी; ताकि अब पश्चिम में शासन कर रही सम्प्रति ने सफलतापूर्वक पाटलिपुत्र में सिंहासन हासिल कर लिया हो, और इस प्रकार साम्राज्य को फिर से एकजुट किया जा सके।
यह घटना 223 ईसा पूर्व में घटी थी। हालाँकि, साम्राज्य का विघटन शायद पहले ही शुरू हो चुका था। जैन स्रोतों में उल्लेख है कि संप्रति ने उज्जैन और पाटलिपुत्र से शासन किया था। दशरथ और संप्रति के बाद सालिसुका नामक एक राजकुमार आया जिसका उल्लेख खगोलशास्त्रीय ग्रंथ गार्गी संहिता में एक दुष्ट झगड़ालू राजा के रूप में किया गया है।
पुराणों के अनुसार सालिसुका के उत्तराधिकारी देववर्मन, सतमधनुस और अंत में बृहद्रथ थे। अंतिम राजकुमार को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने उखाड़ फेंका, जिसने शुंग राजवंश नामक एक नए राजवंश की नींव रखी।
मौर्यों के पतन के कारण:
मगध साम्राज्य, जो कलिंग की विजय में परिणित होने वाले लगातार युद्धों से विकसित हुआ था, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद बिखरना शुरू हो गया। इतनी तीव्र गिरावट के लिए इतिहासकारों द्वारा दिए गए कारण जितने विरोधाभासी हैं उतने ही भ्रमित करने वाले भी हैं।
मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ स्पष्ट और अन्य विवादास्पद कारणों की चर्चा नीचे की गई है:
पतन का एक अधिक स्पष्ट कारण अशोक के बाद कमजोर राजाओं का उत्तराधिकार था।
एक और और तात्कालिक कारण साम्राज्य का दो भागों में विभाजन था, पूर्वी भाग दशरथ के अधीन और पश्चिमी भाग कुणाल के अधीन। यदि विभाजन नहीं हुआ होता, तो उत्तर-पश्चिम में यूनानी आक्रमण को कुछ समय के लिए रोका जा सकता था, जिससे मौर्यों को अपनी पिछली शक्ति को कुछ हद तक फिर से स्थापित करने का मौका मिलता। साम्राज्य के विभाजन ने विभिन्न सेवाओं को भी बाधित कर दिया।
विद्वानों ने सुझाव दिया है कि अशोक की बौद्ध-समर्थक नीतियों और उनके उत्तराधिकारियों की जैन-समर्थक नीतियों ने ब्राह्मणों को अलग-थलग कर दिया और इसके परिणामस्वरूप शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र का विद्रोह हुआ। एच.सी. रायचौधरी का मानना है कि अशोक की शांतिवादी नीतियां साम्राज्य की ताकत को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार थीं।
दूसरा तर्क साम्राज्य और उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए अशोक के अहिंसा पर जोर देने को जिम्मेदार ठहराता है। हरप्रसाद शास्त्री का मानना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन पशु बलि पर प्रतिबंध और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को कम करने के कारण ब्राह्मणवादी विद्रोह का परिणाम था। ये दोनों तर्क काफी सरल हैं।
पुष्यमित्र के सिंहासन पर कब्जे को ब्राह्मण विद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि उस समय तक प्रशासन इतना अप्रभावी हो गया था कि अधिकारी किसी भी व्यवहार्य विकल्प को स्वीकार करने को तैयार थे।
दूसरा प्रस्ताव अहिंसा की नीति की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता है। अशोक के शिलालेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेना को विघटित करने का सुझाव देता हो। इसी प्रकार मृत्युदंड जारी रहा। प्रजातियों की कमी और भोजन के लिए मारे गए जानवरों की संख्या पर जोर दिया गया था। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि जानवरों की हत्या पूरी तरह से बंद हो गई हो।
डी.डी. जैसे कुछ इतिहासकारों द्वारा एक और कारण सामने रखा गया है। कोसंबी का मानना है कि बाद के शासकों के अधीन मौर्य अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव था जिसके कारण भारी कर लगाया गया।
यह राय फिर से एकतरफा है और पुरातात्विक आंकड़ों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़ जैसे स्थलों की खुदाई से भौतिक संस्कृति में सुधार देखा गया है।
मौर्यों के पतन के कारणों में प्रशासन का संगठन और राज्य या राष्ट्र की अवधारणा का बहुत महत्व था। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत चरित्र का था जिसके लिए काफी व्यक्तिगत योग्यता वाले राजा की आवश्यकता थी।
ऐसी स्थिति में केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होने से प्रशासन स्वतः ही कमजोर हो जाता है। अशोक की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारियों की असमान गुणवत्ता के कारण, विशेषकर साम्राज्य के विभाजन के बाद, केंद्र में कमजोरी आ गई।
मौर्य राज्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर कर लगाकर अपना राजस्व प्राप्त करता था, जिसे बढ़ाना और विस्तारित करना होगा ताकि राज्य के प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखा जा सके।
दुर्भाग्य से मौर्यों ने राजस्व क्षमता का विस्तार करने या संसाधनों के पुनर्गठन और पुनर्गठन का कोई प्रयास नहीं किया। मौर्य अर्थव्यवस्था की यह अंतर्निहित कमजोरी अन्य कारकों के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी।
गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रसार के कारण नये राज्यों का निर्माण हुआ।