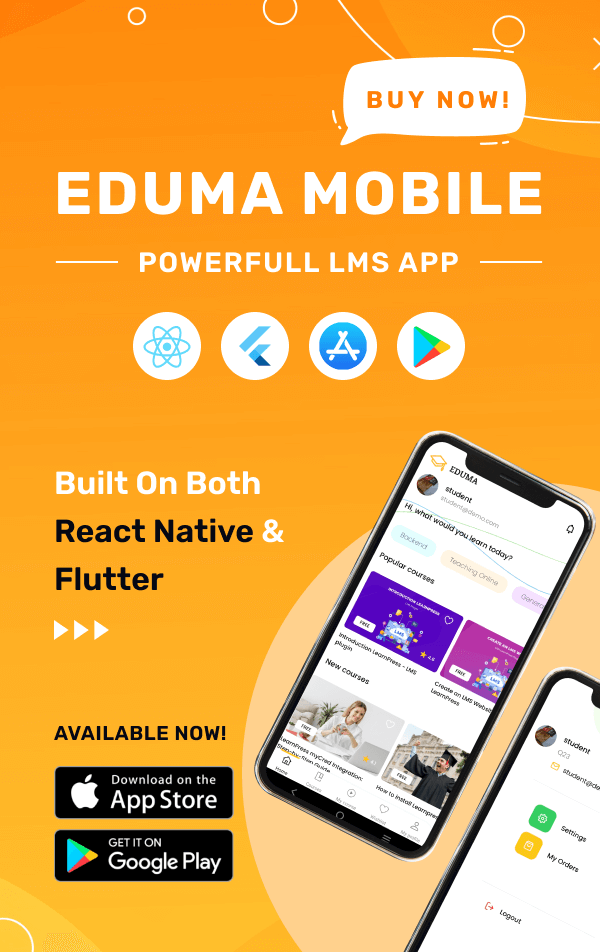पंचायतों
ग्राम पंचायत
पंचायती राज की संरचना में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। यदि इन गाँवों की जनसंख्या बहुत कम हो तो प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह के लिए एक पंचायत होती है। पंचायत में मुख्य रूप से गाँव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
केवल वे व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हैं, पंचायत के चुनाव के लिए पात्र हैं। आपराधिक अपराधों के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति पंचायत के चुनाव से अयोग्य हो जाते हैं।
सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर दो महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को सहयोजित करने का भी प्रावधान है। एक निकाय के रूप में पंचायत गाँव की आम सभा के प्रति जवाबदेह होती है जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, जिसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है। ग्राम पंचायत को अपना बजट, पिछले वर्ष का लेखा-जोखा और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, इसे पंचायत द्वारा लागू किए जाने से पहले ग्राम उत्पादन योजना, कराधान और विकास कार्यक्रमों के प्रस्तावों की बाद की मंजूरी को सुरक्षित करना होगा।
प्रत्येक पंचायत एक अध्यक्ष या सरपंच और एक उपाध्यक्ष या उपसरपंच का चुनाव करती है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव सीधे ग्राम सभा द्वारा या तो हाथ उठाकर या गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है जबकि अन्य राज्यों में चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत व्यवस्था में सरपंच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह पंचायत की विभिन्न गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है। वह पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है और इसके निर्णय लेने के साथ-साथ प्रधान और विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेता है। वह पंचायत के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, पंचायत समिति में इसके प्रवक्ता के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करता है और इसकी गतिविधियों और सहकारी समितियों जैसे अन्य स्थानीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
पंचायत समिति
पंचायत समिति, पंचायती राज में दूसरे स्थान पर है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सभी पहलुओं की जिम्मेदारी लेने के लिए एक एकल प्रतिनिधि और सशक्त लोकतांत्रिक संस्था के रूप में समिति की परिकल्पना की गई है। समिति के अनुसार, समिति “उन कार्यों के लिए पर्याप्त बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है जो ग्राम पंचायत नहीं कर सकती है और फिर भी निवासियों की रुचि और सेवाओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त छोटा है।”
आमतौर पर एक पंचायत समिति में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर 20 से 60 गाँव होते हैं। एक समिति के अंतर्गत औसत जनसंख्या लगभग 80,000 है लेकिन सीमा 35,000 से 1,00,000 तक है। पंचायत समिति में आम तौर पर शामिल होते हैं-
ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के पंचों द्वारा और उनके द्वारा चुने गए लगभग बीस सदस्य;
दो महिला सदस्यों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से एक-एक सदस्य को सह-चयनित किया जाएगा, बशर्ते उन्हें अन्यथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिले;
सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का अनुभव रखने वाले दो स्थानीय व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास के लिए फायदेमंद हो सकते हैं;
ब्लॉक के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों के प्रतिनिधि;
किसी ब्लॉक की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक छोटी नगर पालिका के सदस्यों द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि;
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य और संघ विधानमंडलों के सदस्यों को सहयोगी सदस्यों के रूप में लिया जाना है।
जिला परिषद
जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर है। आम तौर पर, जिला परिषद में पंचायत समिति के प्रतिनिधि होते हैं; राज्य विधानमंडल और संसद के सभी सदस्य, जिले के एक भाग या पूरे का प्रतिनिधित्व करते हैं; चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, अभियांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य विकास विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारी।
इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विशेष प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है, बशर्ते कि उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिले। कलेक्टर जिला परिषद का सदस्य भी होता है।
जिला परिषद का अध्यक्ष इसके सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए सभी राज्यों में जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञ या अधिकारी होते हैं।
जिला परिषद, अधिकांश भाग में, समन्वय और पर्यवेक्षी कार्य करती है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। कुछ राज्यों में जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट को भी मंजूरी देती है। जिला परिषद विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को आवश्यक सलाह भी देती है। यह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों, लघु सिंचाई कार्यों आदि के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। यह स्थानीय उद्योगों और कला को भी बढ़ावा देता है।
जिला परिषद के वित्त में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और भूमि उपकर और अन्य स्थानीय उपकर और करों में हिस्सेदारी शामिल है। कभी-कभी राज्य सरकार द्वारा कुछ कर लगाने या पंचायत समितियों द्वारा पहले से लगाए गए करों को एक निश्चित सीमा के अधीन बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
नगर पालिकाओं
74वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में ‘नगर पालिकाओं’ नामक एक नया भाग IX-A जोड़ा और एक नई बारहवीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है-अनिवार्य और स्वैच्छिक।
कुछ अनिवार्य प्रावधान जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी हैं, वे हैं:
संक्रमणकालीन क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्र), छोटे शहरी क्षेत्रों और बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों का गठन;
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण; महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों तक आरक्षण;
पंचायती राज निकायों में चुनाव कराने के लिए गठित राज्य चुनाव आयोग (73वां संशोधन देखें) शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए भी चुनाव कराएगा;
पंचायती राज निकायों के वित्तीय मामलों से निपटने के लिए गठित राज्य वित्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा;
शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है और पहले विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए चुनाव होने होते हैं;
संघटन
नगर निकायों का गठन नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है) से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से होता है। हालाँकि, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों और विधान परिषद और विधान सभा के सदस्यों को नगरपालिका निकाय में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। राज्य, निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। राज्य विधायिका नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका भी प्रदान कर सकती है। राज्य विधायिका किसी नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका भी प्रदान कर सकती है।
ऐसे समूहों के लिए सीटें आरक्षित करके समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं का सशक्तिकरण संवैधानिक संशोधन के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में से एक है। अध्यक्ष का पद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम की पांच वर्ष की अवधि में से कम से कम एक वर्ष, मेयर का पद एक महिला के लिए आरक्षित है, और एक वर्ष अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। यह नगर पालिकाओं को पांच साल का कार्यकाल देता है और यदि उनमें से किसी को भंग करना है, तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।