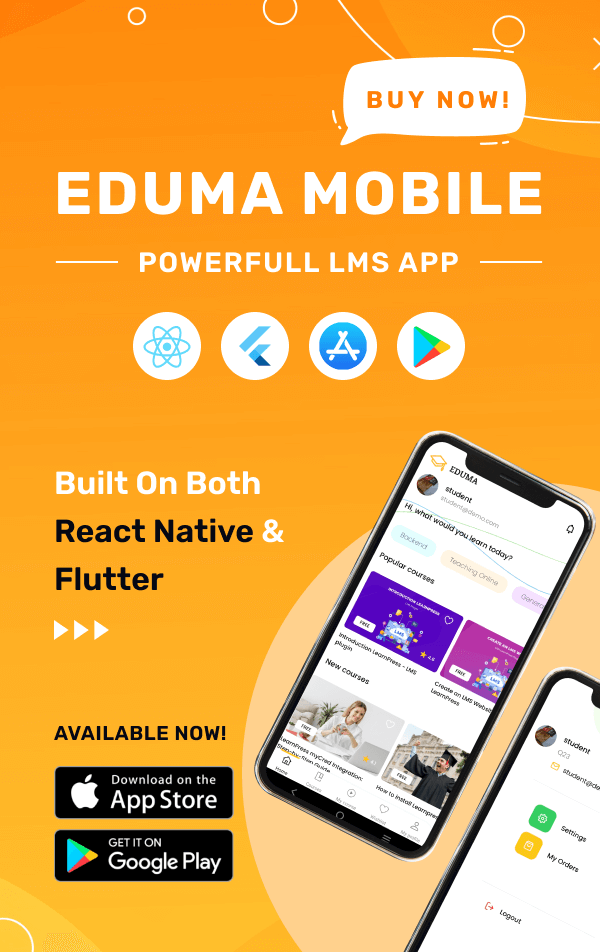शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की जड़ें प्राचीन दुनिया में पाई जाती हैं, जहां सरकारी कार्यों की अवधारणाएं और मिश्रित और संतुलित सरकार के सिद्धांत विकसित हुए थे। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विकास में ये आवश्यक तत्व थे। मध्ययुगीन लेखन के माध्यम से उनके प्रसारण ने, इंग्लैंड में संवैधानिकता के विचारों का आधार प्रदान करने के लिए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को एक वैकल्पिक, लेकिन निकटता से संबंधित, सरकार के हिस्सों की उचित अभिव्यक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाया।
शासन करने की शक्ति को संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वितरित किया जाना चाहिए ताकि एक समूह के पास सारी शक्ति होने से बचा जा सके। प्रत्येक समूह को जिम्मेदारी के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर काम करना चाहिए ताकि प्रत्येक समूह दूसरे के कार्यों पर नज़र रख सके।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी संबंधों से संबंधित है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तीन अंगों के कामकाज में विशिष्टता लाने का प्रयास करता है और इसलिए इस सिद्धांत द्वारा शक्ति का एक सख्त सीमांकन प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह सिद्धांत इस तथ्य को दर्शाता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सरकार की सभी तीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सरकारी कार्यों की जाँच और संतुलन पर आधारित है।
शक्ति पृथक्करण की मुख्य विशेषताएँ हैं:-
एक ही व्यक्ति को सरकार के तीन अंगों में से एक से अधिक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जैसे मंत्रियों को संसद में नहीं बैठना चाहिए;
सरकार के एक अंग को दूसरे अंग द्वारा उसके कार्यों के निष्पादन में नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए या मंत्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए;
सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के कार्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मंत्रियों के पास विधायी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए।
भारत संवैधानिक लोकतंत्र का पालन करता है जो शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण प्रदान करता है। न्यायपालिका शाखा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति के साथ अन्य दो शाखाओं से काफी स्वतंत्र है। संसद के पास विधायी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं जिन्हें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को न केवल संघ सरकार बल्कि संघीय ढांचे में विभिन्न राज्य सरकारों के लिए कार्यपालिका, संसद, सशस्त्र बलों आदि के सामान्य प्रमुख के रूप में संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करने का कर्तव्य सौंपा है। शक्ति संतुलन बनाए रखने और संवैधानिक सीमाओं से आगे न बढ़ने के लिए तीनों शाखाओं में एक-दूसरे पर “नियंत्रण और संतुलन” होता है।
भारत के संविधान के साथ असंगत होने पर राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित कानून या केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को रद्द कर सकता है।
विधायिका द्वारा विधिवत पारित कानून को राष्ट्रपति भी स्वीकार करते हैं, यदि वह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
राष्ट्रपति पर उसके असंवैधानिक आदेशों/निर्णयों के लिए संसद द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के बाद महाभियोग चलाया जा सकता है।
राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक आदेशों/निर्णयों के लिए राष्ट्रपति की पात्रता मानदंड खोने के आधार पर न्यायपालिका द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।
संसद सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर उनकी अक्षमता और दुर्भावना के लिए महाभियोग चला सकती है। न्यायाधीशों की उच्च पीठ संविधान को कायम रखने के लिए न्यायाधीशों की छोटी पीठ के गलत फैसले को रद्द कर सकती है।