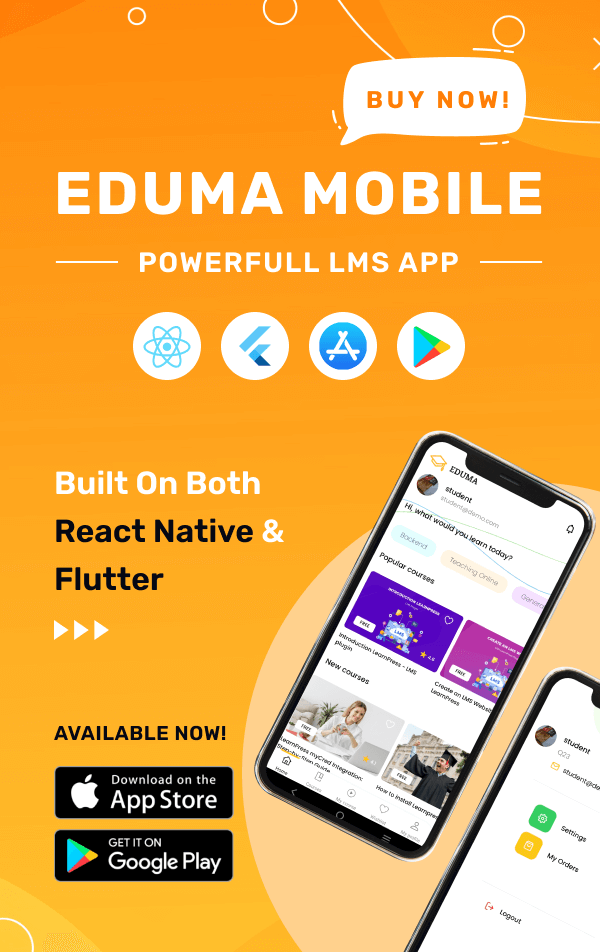सरकार में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सहभागी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त के रूप में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने नागरिकों के प्रति राज्य की नई प्रतिबद्धताओं के रूप में मान्यता मिली। सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में नागरिकों के समर्थन और भागीदारी को सूचीबद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। परंपरागत रूप से, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी और सूचित विकल्प बनाने की क्षमता भारत में एक छोटे अभिजात वर्ग तक ही सीमित रही है। महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर परामर्श, भले ही वे सीधे लोगों से संबंधित हों, शायद ही कभी किया जाता था। सूचना-साझाकरण सीमित होने के कारण, परामर्श प्रक्रिया गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी।
इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सूचना वह मुद्रा है जिसकी प्रत्येक नागरिक को समाज के जीवन और शासन में भाग लेने के लिए आवश्यकता होती है। सूचना तक नागरिकों की पहुंच जितनी अधिक होगी, सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक होगी। वैकल्पिक रूप से, ‘पहुँच’ पर जितने अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ‘शक्तिहीनता’ और अलगाव की भावनाएँ उतनी ही अधिक होती हैं। जानकारी के बिना, लोग नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं या सूचित विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
सरकारी सूचना एक राष्ट्रीय संसाधन है। न तो उस समय की विशेष सरकार, न ही सार्वजनिक अधिकारी, अपने लाभ के लिए जानकारी बनाते हैं। यह जानकारी उनके कार्यालय के कर्तव्यों के वैध निर्वहन से संबंधित उद्देश्यों के लिए और जनता की सेवा के लिए उत्पन्न की जाती है, जिनके लाभ के लिए सरकारी संस्थान मौजूद हैं, और जो अंततः (एक प्रकार के आयात या किसी अन्य के माध्यम से) सरकारी संस्थानों को वित्त पोषित करते हैं। और अधिकारियों का वेतन। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार और अधिकारी लोगों की जानकारी के ‘ट्रस्टी’ हैं।
फिर भी, सैद्धांतिक रूप से, कम से कम ऐसे कई तरीके हैं जिनसे संसदीय प्रणाली में जनता के सदस्यों के लिए जानकारी सुलभ हो सकती है। प्रणालीगत उपकरण सरकार से संसद और विधानमंडलों तक और वहां से लोगों तक सूचना के हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं। जनता के सदस्य अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जानकारी मांग सकते हैं। वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ, समिति रिपोर्ट, सूचना का प्रकाशन और प्रशासनिक कानून आवश्यकताएँ भी सरकार से नागरिक तक सूचना के प्रवाह को बढ़ाती हैं। हाल की तकनीकी प्रगति भी ‘सूचना समृद्ध’ और ‘सूचना’ के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है।
हालाँकि, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत की स्थिति के बावजूद, लोगों को जानकारी का खुलासा करने के लिए गाँव, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हाल तक कोई बाध्यता नहीं थी – जानकारी अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक रहस्य अधिनियम 1923 द्वारा संरक्षित थी, जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक जानकारी का खुलासा करना अपराध है। गोपनीयता, दूरी और रहस्य की औपनिवेशिक विरासत।
एक पार्टी के प्रभुत्व के लंबे इतिहास के साथ मिलकर नौकरशाही पारदर्शिता और प्रभावी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई है, सूचना के प्रभावी अधिकार की तो बात ही छोड़िए, गुप्त सरकार लगभग हमेशा अक्षम होती है क्योंकि यदि समस्याओं का समाधान करना है तो सूचना का मुक्त प्रवाह आवश्यक है। पहचाना और समाधान किया गया।
सूचना के अधिकार को सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने और जन-केंद्रित शासन की शुरुआत करने की कुंजी के रूप में देखा गया है। सूचना तक पहुंच गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है, जिससे उनका कल्याण हो सकेगा। सुशासन के बिना, कोई भी विकासात्मक योजनाएँ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती हैं। सुशासन के चार तत्व हैं- पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमेयता और भागीदारी। पारदर्शिता का तात्पर्य आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में स्पष्टता से है। सूचना का अधिकार सरकार के रिकॉर्ड को सार्वजनिक जांच के लिए खोलता है, जिससे नागरिकों को यह सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मिलता है कि सरकार क्या करती है और कितनी प्रभावी ढंग से करती है, इस प्रकार सरकार अधिक जवाबदेह बनती है। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें अधिक निष्पक्षता से कार्य करने में सक्षम बनाती है जिससे पूर्वानुमानशीलता बढ़ती है। सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी नागरिकों को शासन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में भी सक्षम बनाती है। मूलभूत दृष्टि से सूचना का अधिकार सुशासन की मूलभूत आवश्यकता है।
सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, भारतीय संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (इसके बाद आरटीआई अधिनियम या अधिनियम के रूप में संदर्भित) लागू किया। यह लोगों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला एक पथप्रदर्शक कानून है। जबकि सूचना का अधिकार संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है, अधिनियम नागरिकों के लिए शासन के सभी मामलों पर जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित करता है।
सूचना का अधिकार : चुनौतियाँ
सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सबसे विवादास्पद मुद्दा आधिकारिक रहस्यों से संबंधित है। लोकतंत्र में, लोग संप्रभु होते हैं और चुनी हुई सरकार और उसके पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं। इसलिए चीजों की प्रकृति के अनुसार, शासन के सभी मामलों में पारदर्शिता आदर्श होनी चाहिए। हालाँकि यह अच्छी तरह से माना जाता है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ संवेदनशील मामलों को जनता की नज़र से दूर रखा जाए तो सार्वजनिक हित सबसे अच्छा होता है। इसी प्रकार, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद में सार्वजनिक मुद्दों पर दिन-प्रतिदिन की राजनीति के तनाव और दबाव से मुक्त होकर निर्बाध बहस की मांग करती है। लोगों को कैबिनेट के निर्णयों और उनके कारणों को जानने का निर्बाध अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि वास्तव में ‘कैबिनेट कक्ष’ के दायरे में क्या होता है। अधिनियम राज्य के मामलों में इन गोपनीयता आवश्यकताओं को मान्यता देता है और अधिनियम की धारा 8 ऐसे सभी मामलों को प्रकटीकरण से छूट देती है।
औपनिवेशिक युग के दौरान अधिनियमित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (बाद में ओएसए के रूप में संदर्भित), शासन में गोपनीयता और गोपनीयता के सभी मामलों को नियंत्रित करता है। यह कानून मुख्य रूप से सुरक्षा के मामलों से संबंधित है और जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर अन्य हमलों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हालाँकि, लोगों के प्रति अविश्वास के औपनिवेशिक माहौल और नागरिकों से निपटने में सार्वजनिक अधिकारियों की प्रधानता को देखते हुए, ओएसए ने गोपनीयता की संस्कृति बनाई। गोपनीयता आदर्श बन गई और खुलासा अपवाद। जबकि ओएसए की धारा 5 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों से निपटना था, कानून की शब्दावली और औपनिवेशिक काल में जब इसे लागू किया गया था, तो इसने इसे व्यावहारिक रूप से शासन के हर मुद्दे को एक गोपनीय मामले में परिवर्तित करने वाला एक कानूनी प्रावधान बना दिया। . इस प्रवृत्ति को सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 द्वारा बल मिला, जो बिना प्राधिकरण के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ के संचार पर रोक लगाता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि 1872 में अधिनियमित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, विभाग के प्रमुख की अनुमति के बिना अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से साक्ष्य देने पर रोक लगाती है, जिनके पास इस मामले में प्रचुर विवेक है। कहने की जरूरत नहीं है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों के वर्गीकरण के लिए जारी किए गए निर्देशों और आधिकारिक प्रक्रियाओं ने भी जानकारी को रोकने की इस प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें आधिकारिक रहस्यों से संबंधित प्रावधान हों।
सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
अधिकारों को लागू करने और अधिनियम के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए संस्थानों का निर्माण, सूचना का संगठन और एक सक्षम वातावरण का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसलिए, आयोग ने पहले कदम के रूप में अधिनियम को लागू करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की निम्नानुसार समीक्षा की है:
संस्थानों
सूचना आयोग
सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी।
सूचना एवं रिकार्ड रखना
धारा के तहत स्वत: संज्ञान घोषणा
जनहित प्रकटीकरण.
रिकार्डकीपिंग का आधुनिकीकरण
क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन
निगरानी तंत्र का निर्माण
क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन
प्रशिक्षण कार्यक्रम: सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम है। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि मांगी गई जानकारी शीघ्रता से और सुगम रूप में प्रदान की जाए। सरकारी पदाधिकारियों की मानसिकता, जिसमें गोपनीयता आदर्श है और खुलासा अपवाद है, में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। ऐसे बदलाव की आवश्यकता उन नागरिकों की मानसिकता में भी होगी जो परंपरागत रूप से जानकारी प्राप्त करने में अनिच्छुक रहे हैं। इस आमूलचूल परिवर्तन को लाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। चुनिंदा सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने में आयोग के अपने अनुभव से पता चलता है कि कुछ पीआईओ भी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से परिचित नहीं हैं। यूनाइटेड किंगडम में सूचना आयुक्त कार्यालय ने सार्वजनिक अधिकारियों और विशेष रूप से उन कर्मचारियों की सहायता के लिए एक ‘जागरूकता मार्गदर्शन’ श्रृंखला प्रकाशित की है, जिनके पास कुछ मुद्दों, विशेष रूप से छूट प्रावधानों के बारे में विशेषज्ञ सलाह तक पहुंच नहीं है। यह प्रथा भारत में भी अपनाई जा सकती है।
जागरूकता सृजन: सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने से मीडिया में सूचना की स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर गहन बहस छिड़ गई है। इसके बावजूद, पूछताछ से पता चलता है कि जागरूकता का स्तर, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, आश्चर्यजनक रूप से कम है। अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि नागरिक अपने अधिकारों और शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इस अधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हों। अब तक जागरूकता सृजन मुख्यतः प्रिंट मीडिया में सरकारी विज्ञापन तक ही सीमित रहा है। एक प्रभावी जागरूकता सृजन अभियान में नुक्कड़ नाटक, टेलीविजन स्पॉट, रेडियो जिंगल और अन्य जन संचार तकनीकों सहित मल्टी मीडिया प्रयास शामिल होने चाहिए। रचनात्मकता, जुनून और व्यावसायिकता वाले प्रतिबद्ध स्वैच्छिक संगठनों और कॉरपोरेट्स को शामिल करने पर इन अभियानों को कम लागत पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है।
कार्यान्वयन में मुद्दे
आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन एक प्रशासनिक चुनौती है जिसने विभिन्न संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों और समस्याओं को जन्म दिया है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
पहुंच को सुगम बनाना: जानकारी मांगने के लिए, अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को गति में स्थापित करना होगा। ट्रिगर एक अनुरोध दाखिल करना है। एक बार अनुरोध दायर हो जाने के बाद इसका जवाब देने की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी पर आ जाती है। अनुभवों के आधार पर कार्यान्वयन में कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं:
अनुरोध स्वीकार करने की जटिल प्रणाली।
डिमांड ड्राफ्ट पर जोर.
डाक द्वारा आवेदन दाखिल करने में कठिनाइयाँ।
आवेदन शुल्क की दरें बदलती और अक्सर ऊंची होती हैं।
बड़ी संख्या में पीआईओ.
अनुरोध स्वीकार करने की जटिल प्रणाली: आवेदन स्वीकार करते समय विभाग इस बात पर ज़ोर देते हैं कि नकद भुगतान लेखा कार्यालय में किया जाए। मंत्रालयों में, लेखा कार्यालय और पीआईओ कार्यालय अलग-अलग होते हैं और कभी-कभी अलग-अलग स्थानों पर होते हैं। नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि सूचना के प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए रु. 2 का भुगतान करना होगा, जिसके लिए आवेदक को इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों में कठिनाई और अधिक बढ़ जाएगी, जिनमें से कई में नकदी एकत्र करने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, किसी सरकारी भवन में प्रवेश करने के लिए आगंतुक पास प्राप्त करने से अनुचित प्रतीक्षा समय लगता है (विशेषकर, जब जिम्मेदार पीआईओ कई अन्य जिम्मेदारियों के कारण उपलब्ध नहीं हो सकता है जिन्हें वह संभालता है)। इसलिए, सूचना के लिए अनुरोध दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।
डिमांड ड्राफ्ट पर जोर: हालांकि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन यह एक और समस्या पैदा करता है, क्योंकि बैंक 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 35 रुपये का शुल्क लेता है। इसलिए कुछ विभागों द्वारा केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क प्राप्त करने का आग्रह किया जाता है। और नकदी से दूर रहने की जरूरत नहीं है।
डाक द्वारा आवेदन दाखिल करने में कठिनाइयाँ: मौजूदा व्यवस्था के तहत, डाक द्वारा आवेदन दाखिल करने में आवश्यक रूप से डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान शामिल होगा।
आवेदन शुल्क की अलग-अलग और अक्सर उच्च दरें: विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। तमिलनाडु सूचना का अधिकार (शुल्क) नियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक अनुरोध के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। चेन्नई में अपनी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, आयोग को सूचित किया गया कि शुल्क की इस उच्च दर ने अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने को हतोत्साहित किया है। इसलिए शुल्क संरचना में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
सुझाव
भुगतान के मौजूदा तरीकों के अलावा, उपयुक्त सरकारों को पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भुगतान को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन करना चाहिए।
राज्यों को आवेदन शुल्क के संबंध में ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता हो सकती है जो केंद्रीय नियमों के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शुल्क स्वयं हतोत्साहित न हो जाए।
उपयुक्त सरकारें 5 रुपये के गुणकों में फीस (अतिरिक्त शुल्क सहित) का पुनर्गठन कर सकती हैं। रुपये का शुल्क निर्धारित करने के बजाय। प्रति अतिरिक्त पृष्ठ 2 रुपये का शुल्क रखना वांछनीय हो सकता है। प्रत्येक 3 पेज या उसके भाग के लिए 5}।
राज्य सरकारें शुल्क के भुगतान के तरीके के रूप में उपयुक्त मूल्यवर्ग में उचित टिकट जारी कर सकती हैं। ऐसे टिकटों का उपयोग राज्य सरकारों के दायरे में आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष आवेदन करने के लिए किया जाएगा।
चूंकि देश के सभी डाकघरों को पहले से ही केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से एपीआईओ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए उन्हें नकद में शुल्क एकत्र करने और आवेदन के साथ रसीद अग्रेषित करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है।
भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में चिन्हित किया गया है। इस नोडल विभाग के पास उन सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पूरी सूची होनी चाहिए जो सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के पास उसके दायरे में आने वाले सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की एक विस्तृत सूची भी होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों को (i) संवैधानिक निकायों, (ii) लाइन एजेंसियों, (iii) वैधानिक निकायों, (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, (v) कार्यकारी आदेशों के तहत बनाए गए निकायों, (vi) में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन। प्रत्येक श्रेणी के भीतर सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की एक अद्यतन सूची बनाए रखनी होगी।
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास तत्काल अगले स्तर पर उसके अधीनस्थ सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का विवरण होना चाहिए। यह अंतिम स्तर तक पहुंचने तक जारी रहना चाहिए। ये सभी विवरण संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर पदानुक्रमित रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
ऐसी ही व्यवस्था राज्यों को भी अपनानी चाहिए।
चुनाव नागरिकों के लिए अपने देश के अधिकारियों को कार्यालय में उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का प्राथमिक साधन है, खासकर जब उन्होंने सरकार के काम को पूरा करने में अवैध, भ्रष्ट या अयोग्य व्यवहार किया हो। चुनावों के लिए – और लोगों की इच्छा – सार्थक होने के लिए, बुनियादी अधिकारों की रक्षा और पुष्टि की जानी चाहिए, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विधेयक के माध्यम से किया जाता है। बिल ऑफ राइट्स के लेखक जेम्स मैडिसन का मानना था कि सरकार की प्रतिक्रिया का मूल आधार यह आश्वासन था कि नागरिकों के पास इसे निर्देशित करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होगा। यदि नागरिकों को सीधे या प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करना है, तो उन्हें अपने मामलों को सर्वोत्तम तरीके से निर्धारित करने के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से सूचित नहीं किया जाता है, तो वे मोटे तौर पर न तो अपने स्वार्थ में कार्य कर सकते हैं, न ही उनके पास चुनावों में कोई गंभीर विकल्प हो सकता है, खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश करना तो दूर की बात है।