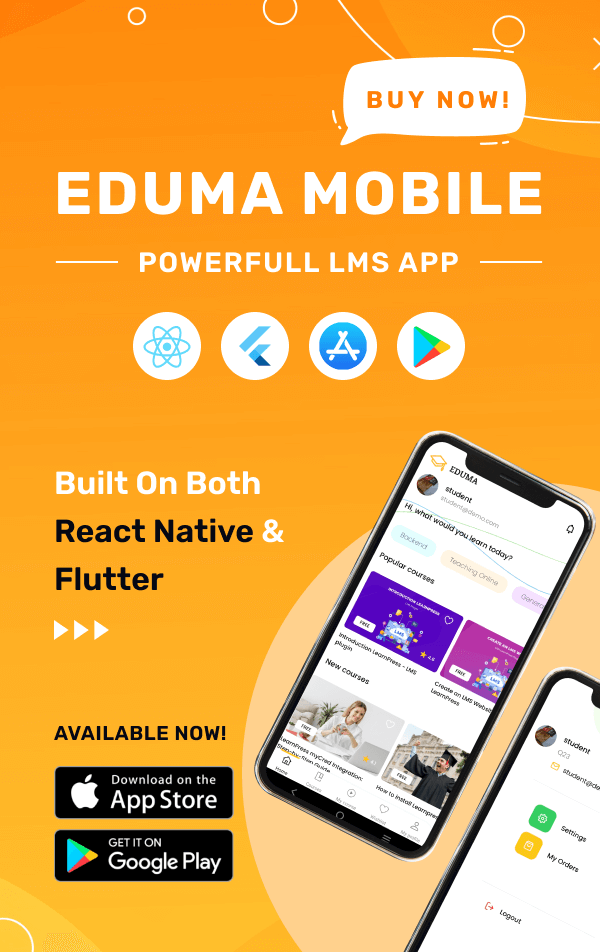सरकार का संसदीय स्वरूप सरकार की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायी विभागों के बीच घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध मौजूद होता है और कार्यकारी विभाग की स्थिरता और प्रभावकारिता विधायिका पर निर्भर करती है। कानून बनाने और लागू करने का अधिकार संसद के पास है।
हालाँकि संसदीय सरकार को मोटे तौर पर उपरोक्त तरीके से परिभाषित किया गया है, ऐसी प्रणाली में अब विधायिका की सर्वोच्चता का स्थान मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता ने ले लिया है। इसलिए, इस प्रकार की सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है।
सरकार के संसदीय स्वरूप में, राज्य का मुखिया आमतौर पर सरकार के मुखिया से अलग व्यक्ति होता है। एक सम्राट या राष्ट्रपति आमतौर पर राज्य का प्रमुख होता है। हालाँकि, वह राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख नहीं। राज्य के मुखिया के कार्य मुख्यतः औपचारिक या औपचारिक होते हैं। मंत्रिपरिषद या कैबिनेट सरकार चलाने के लिए वास्तविक कार्यकारी शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करती है। कई देशों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
संसदीय या कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। सरकार का यह स्वरूप ब्रिटेन, भारत और कनाडा जैसे देशों में मौजूद है। सरकार के इस संसदीय स्वरूप को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है।
विशेषताएँ
सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है:
एक नामधारी या संवैधानिक शासक का अस्तित्व: संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता एक नामधारी संवैधानिक शासक का अस्तित्व है। कानूनी तौर पर राज्य के सभी मामलों का प्रशासन राज्य के मुखिया द्वारा संचालित किया जाता है। हालाँकि, वास्तव में, प्रशासन मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है। सम्राट या राष्ट्रपति, जैसा भी मामला हो, राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख नहीं।
शक्तियों के पृथक्करण का अभाव: संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया जाता है। यहां सरकार के तीन विभाग एक-दूसरे की कुछ शक्तियों और कार्यों को साझा करते हुए, निकट, घनिष्ठ संपर्क में काम करते हैं।
मंत्रालय-गठन में निचले सदन की मुख्य भूमिका: संसदीय सरकार में विधानमंडल का निचला सदन, यानी लोकप्रिय सदन, मंत्रालय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सदन में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधान मंत्री या चांसलर नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक शासक अपनी सलाह पर मंत्रालय के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व: ऐसी प्रणाली में मंत्रिमंडल या मंत्रालय को अपनी सभी गतिविधियों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। द्विसदनीय विधायिका वाले देशों में मंत्रिमंडल जनता के प्रतिनिधियों से बने निचले सदन के प्रति उत्तरदायी रहता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व: विधायिका के प्रति मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व पुनः दो प्रकार का हो सकता है:
व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और सामूहिक जिम्मेदारी.
व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब है कि किसी विभाग के प्रभारी मंत्री को अपने विभाग की गतिविधियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन जब मंत्री सरकार की नीतियों और गतिविधियों के लिए विधायिका के प्रति संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहते हैं, तो इसे ‘सामूहिक जिम्मेदारी’ कहा जाता है। चूँकि कोई भी व्यक्तिगत मंत्री कैबिनेट की सहमति के बिना सरकार का कोई भी कार्य एकतरफा नहीं कर सकता, इसलिए पूरे मंत्रालय या कैबिनेट को संबंधित मंत्री की त्रुटियों के लिए जवाबदेह रहना पड़ता है।
विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध: संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायी विभागों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए वे एक-दूसरे को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। विधायिका में बहुमत दल या गठबंधन के नेता मंत्रिमंडल या मंत्रालय के सदस्य बनते हैं। स्वाभाविक रूप से, मंत्री आसानी से विधायिका पर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। नतीजतन, मंत्रिमंडल के कार्यक्रमों और नीतियों को विधायिका के अंदर बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।
प्रधानमंत्री का नेतृत्व: प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता है। विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधान मंत्री बनता है। हालाँकि, सिद्धांत रूप में, वह ‘प्राइमस इंटर पेर्स’ हैं, यानी ‘बराबरों में प्रथम’, वास्तव में, उनके पास अन्य मंत्रियों की तुलना में बहुत अधिक शक्ति और स्थिति है। विधानमंडल में बहुमत दल या गठबंधन के निर्विवाद नेता के रूप में वह सरकारी नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल, संसदीय लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, कार्यकुशलता और करिश्मा पर निर्भर करती है।
एक मजबूत विपक्ष का अस्तित्व: एक या एक से अधिक मजबूत और सुसंगठित विपक्षी दल या पार्टियों का अस्तित्व संसदीय प्रणाली की पहचान है। सरकार की त्रुटियों की आलोचना करके विपक्ष उसे कल्याणकारी उपाय अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है और उसे निरंकुश होने से रोक सकता है। इस दृष्टि से देखें तो विपक्ष को संसदीय लोकतंत्र की प्राणशक्ति कहा जा सकता है।
कैबिनेट तानाशाही: सरकार की संसदीय प्रणाली में कैबिनेट को कई कार्य करने होते हैं।
यह मंत्रिमंडल है जो:
सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों की समीक्षा करके सुविचारित नीतियां बनाती है, उसके द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून पारित करने की व्यवस्था करती है, केंद्रीय विधायिका के एजेंडे में शामिल किए जाने वाले मामलों का निर्धारण करती है, नियंत्रण और निर्देशन करती है प्रशासनिक विभाग ताकि कानूनों, सरकारी आदेशों आदि को ठीक से लागू किया जा सके, सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय किया जाता है, प्रधान मंत्री के परामर्श से मसौदा बजट तैयार किया जाता है और इसे विधायिका में पारित कराने के लिए आवश्यक पहल की जाती है। आर्थिक नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, आपातकाल या अप्रत्याशित स्थिति के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक प्रमुख को सलाह देता है, आदि। इस तरह मंत्रिमंडल ‘राजनीतिक आर्क की आधारशिला’ के रूप में कार्य करता है या ‘संचालन’ बन गया है राज्य के जहाज का पहिया’ वास्तव में, सरकार की संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सदस्य विधायिका में बहुमत दल या गठबंधन के नेता होते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि संसद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे एक प्रकार की “कैबिनेट तानाशाही” को बढ़ावा मिलता है।
लाभ :
सरकार का संसदीय स्वरूप बहुत सारे लाभ प्रदान करता है: कार्यपालिका और विधायी अंगों के बीच घनिष्ठ सहयोग से सरकार का कामकाज सुचारू होता है और उनके बीच अनावश्यक टकराव से बचा जा सकता है। ये दोनों अंग परस्पर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
सरकार की जिम्मेदारी एक खुला प्रशासन सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका, अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार रहने और प्रशासन से संबंधित विधायिका के प्रश्नों का उनकी संतुष्टि के लिए उत्तर देने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहती है, हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करती है, क्योंकि यह उसकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करता है। जितनी अधिक गलती, चुनाव में लोकप्रिय समर्थन की संभावना उतनी ही कम होगी।
प्रणाली लचीली है. लचीलापन किसी भी प्रणाली में एक परिसंपत्ति है क्योंकि यह समायोजन के लिए जगह प्रदान करता है। सरकार का संसदीय स्वरूप बदलती परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुकूल है। उदाहरण के लिए गंभीर आपातकाल के समय परिस्थितियों से निपटने के लिए नेतृत्व को बिना किसी परेशानी के बदला जा सकता है जैसा कि इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। श्री चेम्बरलेन ने युद्ध को संभालने के लिए श्री विंस्टन चर्चिल के लिए रास्ता बनाया। यहां तक कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक चुनाव भी टाला जा सकता है. प्रणाली में ऐसा लचीलापन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मौजूद नहीं है जो अत्यधिक कठोर है।
इस प्रणाली के तहत प्रशासन में खामियों के लिए जिम्मेदारी का पता लगाना आसान है। सिविल सेवकों का एक विशाल समूह है जो स्थायी कार्यपालिका का गठन करता है। वास्तव में वे राजनीतिक आकाओं को प्रशासन की नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में मदद करते हैं। लेकिन यह राजनीतिक नेतृत्व या कैबिनेट है जो प्रशासन में हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए कहा जाता है कि नौकरशाही मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी की आड़ में फलती-फूलती है।
सिस्टम की एक बड़ी खूबी, जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने बताया है, निर्णय लेने में तेजी है। कार्यपालिका कोई भी निर्णय ले सकती है और उसे बिना किसी बाधा के शीघ्र क्रियान्वित कर सकती है। चूंकि सत्ता में रहने वाली पार्टी को विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह निराश होने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है।
यह मंत्रिमंडल है जो:
सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों की समीक्षा करके सुविचारित नीतियां बनाती है, उसके द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून पारित करने की व्यवस्था करती है, केंद्रीय विधायिका के एजेंडे में शामिल किए जाने वाले मामलों का निर्धारण करती है, नियंत्रण और निर्देशन करती है प्रशासनिक विभाग ताकि कानूनों, सरकारी आदेशों आदि को ठीक से लागू किया जा सके, सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय किया जाता है, प्रधान मंत्री के परामर्श से मसौदा बजट तैयार किया जाता है और इसे विधायिका में पारित कराने के लिए आवश्यक पहल की जाती है। आर्थिक नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, आपातकाल या अप्रत्याशित स्थिति के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक प्रमुख को सलाह देता है, आदि। इस तरह मंत्रिमंडल ‘राजनीतिक आर्क की आधारशिला’ के रूप में कार्य करता है या ‘संचालन’ बन गया है राज्य के जहाज का पहिया’ वास्तव में, सरकार की संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सदस्य विधायिका में बहुमत दल या गठबंधन के नेता होते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि संसद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे एक प्रकार की “कैबिनेट तानाशाही” को बढ़ावा मिलता है।
लाभ :
सरकार का संसदीय स्वरूप बहुत सारे लाभ प्रदान करता है: कार्यपालिका और विधायी अंगों के बीच घनिष्ठ सहयोग से सरकार का कामकाज सुचारू होता है और उनके बीच अनावश्यक टकराव से बचा जा सकता है। ये दोनों अंग परस्पर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
सरकार की जिम्मेदारी एक खुला प्रशासन सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका, अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार रहने और प्रशासन से संबंधित विधायिका के प्रश्नों का उनकी संतुष्टि के लिए उत्तर देने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहती है, हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करती है, क्योंकि यह उसकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करता है। जितनी अधिक गलती, चुनाव में लोकप्रिय समर्थन की संभावना उतनी ही कम होगी।
प्रणाली लचीली है. लचीलापन किसी भी प्रणाली में एक परिसंपत्ति है क्योंकि यह समायोजन के लिए जगह प्रदान करता है। सरकार का संसदीय स्वरूप बदलती परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुकूल है। उदाहरण के लिए गंभीर आपातकाल के समय परिस्थितियों से निपटने के लिए नेतृत्व को बिना किसी परेशानी के बदला जा सकता है जैसा कि इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। श्री चेम्बरलेन ने युद्ध को संभालने के लिए श्री विंस्टन चर्चिल के लिए रास्ता बनाया। यहां तक कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक चुनाव भी टाला जा सकता है. प्रणाली में ऐसा लचीलापन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मौजूद नहीं है जो अत्यधिक कठोर है।
इस प्रणाली के तहत प्रशासन में खामियों के लिए जिम्मेदारी का पता लगाना आसान है। सिविल सेवकों का एक विशाल समूह है जो स्थायी कार्यपालिका का गठन करता है। वास्तव में वे राजनीतिक आकाओं को प्रशासन की नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में मदद करते हैं। लेकिन यह राजनीतिक नेतृत्व या कैबिनेट है जो प्रशासन में हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए कहा जाता है कि नौकरशाही मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी की आड़ में फलती-फूलती है।
सिस्टम की एक बड़ी खूबी, जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने बताया है, निर्णय लेने में तेजी है। कार्यपालिका कोई भी निर्णय ले सकती है और उसे बिना किसी बाधा के शीघ्र क्रियान्वित कर सकती है। चूंकि सत्ता में रहने वाली पार्टी को विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह निराश होने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है।