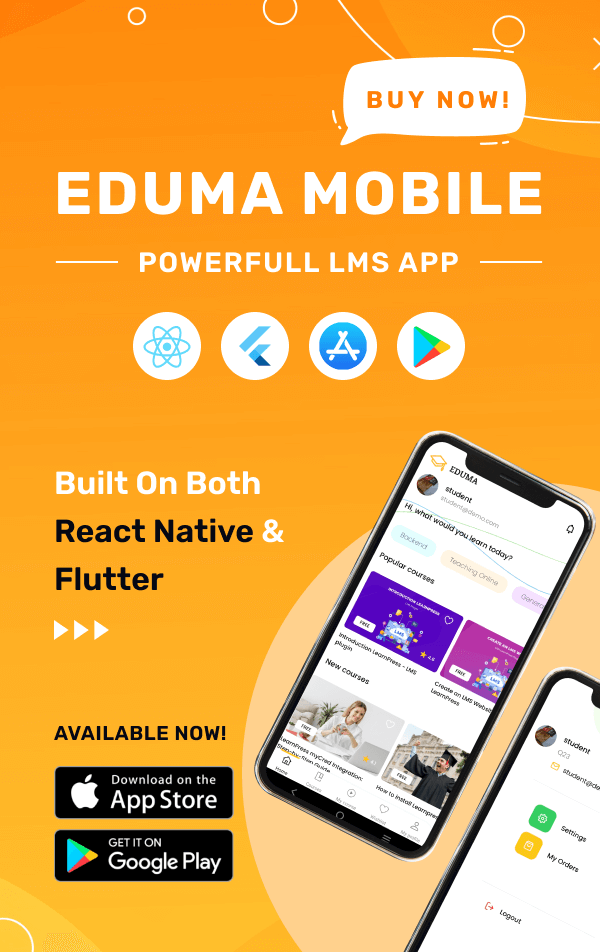यद्यपि ऋग्वेद धार्मिक प्रकृति के भक्ति कार्य से संबंधित है, फिर भी यह प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एक ज्वलंत चित्र देता है। वैदिक सभ्यता को सामाजिक जीवन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक जीवन और धार्मिक मान्यताओं से सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई थी। कुल का नेतृत्व कुलपा करता था, जो आमतौर पर सबसे बड़ा सदस्य होता था। समाज मूलतः पितृसत्तात्मक था और पुत्र के जन्म की बार-बार इच्छा की जाती थी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। बहुविवाह और बहुपति प्रथा दोनों प्रचलन में थे।
वर्ण व्यवस्था का विकास
हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक स्तर विद्यमान थे। इसी प्रकार ईरानी समाज में भी समाज का तीन गुना विभाजन {पुजारी, शासक और उत्पादक} था। हालाँकि, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ हुआ वह अद्वितीय और असाधारण था। उत्तर वैदिक युग में राजसत्ता के विकास में, पुजारियों (ब्राह्मण) और शासकों (क्षत्रिय) ने समाज में अपनी-अपनी स्थिति मजबूत कर ली। निर्माता दो गुटों में बंट गये. स्वतंत्र किसानों और व्यापारियों ने वैश्य समूह बनाया, जबकि दास, मजदूर, कारीगर चौथे समूह शूद्र में बदल गए। यह प्रारंभ में व्यवसाय पर आधारित था लेकिन बाद में जन्म के आधार पर कठोर हो गया। छोटी आबादी के बावजूद, लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन चार समूहों में विभाजित हो गए।
विवाह और महिलाएं
परिवार के पितृसत्तात्मक चरित्र के बावजूद, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बाद के समय की तुलना में बहुत बेहतर थी। वे सभाओं में उपस्थित हो सकती थीं और अपने पतियों के साथ बलिदान चढ़ा सकती थीं। भजनों के रचयिता के रूप में पाँच महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें से घोषा, लोपामुद्रा और अपाला प्रसिद्ध हैं। लड़कियों की शादी आम तौर पर युवावस्था के बाद (16 से 17 साल की उम्र के बीच) कर दी जाती थी। अविवाहित लड़कियाँ अपने माता-पिता के घर में पली-बढ़ीं। विश्ववारा और अपाला जैसी कुछ अविवाहित महिलाओं ने स्वयं बलिदान दिया। ऋग्वेद में भी विधवा पुनर्विवाह के प्रमाण मिलते हैं।
शिक्षा
प्रारंभिक ऋग्वैदिक युग में संपूर्ण शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। ऐसा लगता है कि लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में बुद्धि की उत्तेजना के लिए सावित्री से प्रार्थना है। महिला शिक्षक भी थीं. उनमें से कई लोगों के पास उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान था। मैत्रेयी और गार्गी प्रतिभाशाली विद्वान थीं। ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक मंत्र सीखने का अधिकार था। उत्तर-वैदिक चरण में, वर्णाश्रम के विकास के साथ, शिक्षा अलंकरण समारोह (उपनयन) के साथ शुरू हुई। चूँकि उपनयन तीन उच्च वर्णों तक ही सीमित था, इसलिए शूद्र शिक्षा के हकदार नहीं थे। कभी-कभी लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाता था। जब शिक्षक छात्र से संतुष्ट हो जाता था, तो अंतिम उपदेश दिया जाता था, जिसे स्नाटकोपदेश (एक प्रकार का दीक्षांत समारोह) कहा जाता था।
गोत्र संस्था
गोत्र या गौपेन सामाजिक संबंधों को व्यापक बनाने का एक तंत्र था, अब तक असंबद्ध लोगों के बीच एक नया संबंध स्थापित किया गया था। यह संभव है कि जानवरों को सामूहिक रूप से चराया जाता था और ऐसे स्थान को गोत्र के रूप में जाना जाता था और इससे इसने एक बहिर्विवाही संस्था का चरित्र प्राप्त कर लिया।
आमोद-प्रमोद और मनोरंजन
संगीत, स्वर और वाद्य दोनों, प्रसिद्ध थे। वैदिक आर्य ढोल और झांझ के साथ वीणा और बांसुरी बजाते थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी। नाचना आम बात थी. रथ दौड़ एक पसंदीदा खेल और मनोरंजन का साधन था। रथ दौड़ राजा के राजनीतिक अधिकार का एक प्रतीकात्मक स्रोत थी। जुए के प्रति आकर्षण और इसकी लत से होने वाली बर्बादी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
घर संभालना
गृह सूत्र एक आचार संहिता निर्धारित करता है, जो उत्तर-वैदिक युग के शिष्टाचार और शिष्टाचार का काफी अच्छा विचार देता है। अतिथि (अतिथि) का हर समय स्वागत किया जाता था और विशेष अतिथियों, जैसे गुरु, राजा और ससुर आदि को विशेष उपचार दिया जाता था। बड़ों का सम्मान, आत्म-संयम, नैतिक शुद्धता, सभी प्रकार के संयम और निष्ठा कुछ ऐसे गुण थे। स्वच्छता एक जुनून था. दैनिक स्नान, समय-समय पर पैरों और हाथों को धोना और वैदिक मंत्रों के साथ वातावरण को शुद्ध करना अनुष्ठान का एक हिस्सा था जब उत्तर-वैदिक युग में कर्मकांड ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया था। यह ब्राह्मणों के लिए पदानुक्रम और सर्वोच्चता के विकास के कई स्रोतों में से एक बन गया।
भोजन संबंधी आदतें
प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों द्वारा उत्पादित मुख्य अनाज यवा या जौ था। गेहूँ (गोधुमा) केवल बाद के वैदिक ग्रंथों में ही मिलता है। यवा भी विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए एक सामान्य शब्द था। जैसे, दुग्ध उत्पाद और मवेशी का मांस उनके भोजन की आदतों में शामिल थे। अल्कोहलिक/गैर-अल्कोहलिक पेय ज्ञात और आम थे। सोमा और सुरा दो लोकप्रिय शराब हैं। सुरा एक प्रकार की बीयर या वाइन हो सकती है।
ड्रेस कोड
आम तौर पर कपड़े के दो टुकड़े पहने जाते थे – ऊपरी वस्त्र को उत्तरीय कहा जाता था और निचले को अंतरिया कहा जाता था। पुरुष और महिला की पोशाक में ज्यादा अंतर नहीं था।
स्वास्थ्य और सफ़ाई
सभी की अभिलाषा थी और सभी को सौ वर्ष तक जीने का आशीर्वाद मिला। मिर्गी आम बात थी और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता था। बीमारियों को ठीक करने के लिए अंधविश्वास और जादुई जादू का सहारा लिया जाता था। चमत्कारी इलाज का श्रेय जुड़वां देवताओं, अश्विनों को दिया जाता है, जो रोगों के महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सा कला में विशेषज्ञ हैं। वे दिव्य चिकित्सक थे जिन्होंने आंखों की रोशनी बहाल की और अंधे, बीमार और अपंगों को ठीक किया।
ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था
ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः देहाती थी। उन्होंने मृग यानी जंगली जानवरों के विपरीत पाशु (जिसमें मवेशी, घोड़े और यहां तक कि इंसान भी शामिल थे) को पालतू बनाया। मवेशी धन का पर्याय थे और धनवान व्यक्ति को गोमट कहा जाता था। मवेशी इतने महत्वपूर्ण थे कि युद्ध की शर्तें गौ से ही बनीं, जैसे गविष्टि, गोसु, गव्यट, गव्यु। गोधूलि समय का मापक था। राजा को गोप और गोपति विशेषण दिये जाते थे। दुहित्री शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था क्योंकि वह गाय का दूध निकालती थी। देवताओं की चार श्रेणियों में से एक को गोजटा के नाम से जाना जाता था, यानी गाय का बच्चा। जब वैदिक लोगों का सामना भैंस से हुआ, तो उन्होंने उसे गौरी और गवला या गाय-बाल कहा। छापों में प्राप्त मवेशियों को परिवारों के बीच बाँट दिया गया। मवेशी दान की एक महत्वपूर्ण वस्तु थे और यह बलि का एक हिस्सा भी हो सकता था, जो कबीले या विस सदस्यों द्वारा राजा को दी जाने वाली श्रद्धांजलि थी। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः मवेशी और विशेष रूप से गाय विनिमय का मुख्य माध्यम थे। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। लोग बुआई, कटाई, मड़ाई और विभिन्न कृषि मौसमों से अच्छी तरह परिचित थे। लोग पशुपालक थे, गाय पूजनीय थी लेकिन गायों और बैलों की बलि भी दी जाती थी। पुजारियों को उपहार गायों और महिला दासों की संख्या के संदर्भ में थे, लेकिन भूमि की माप के अनुसार नहीं।
शिल्प और धातुकर्म
सभी प्रकार के शिल्पों का अभ्यास किया जाता था। वहाँ कुम्हार, रथ निर्माता, बढ़ई, बुनकर और चमड़े के कारीगर थे। धातु का काम इस प्रकार जाना जाता था: तांबे को “अयस” के नाम से जाना जाता था, सोने को हिरण्य के नाम से जाना जाता था, लोहे को श्यामा या कृष्ण अयस के नाम से भी जाना जाता था।
धर्म
मन्दिर जैसे कोई पूजा स्थल नहीं थे। ऋग्वेद में “नश्वर हाथों से बनाए गए मंदिरों” और पूजा स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित होने का कोई संकेत नहीं है। इसके विपरीत, प्रत्येक गृहस्थ, अपने परिवार के प्रत्येक पितृपुरुष ने अपने घर में यज्ञ अग्नि जलाई और सोम रस की आहुतियाँ डालीं और देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली, प्रचुर फसल और धन और मवेशियों के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। बीमारी, और काले आदिवासियों पर विजय के लिए। प्राकृतिक घटनाओं की कल्पना विभिन्न देवताओं के कुछ आध्यात्मिक भिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी।